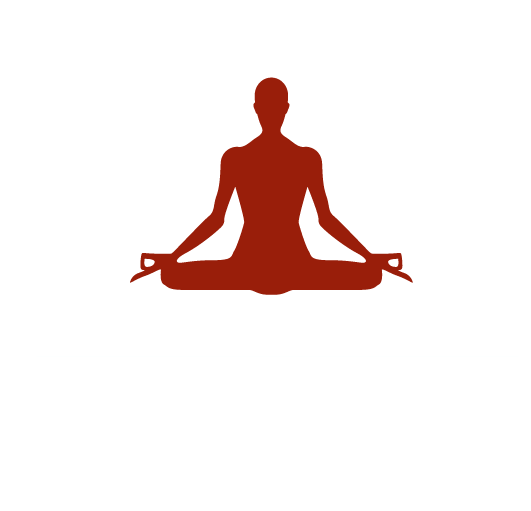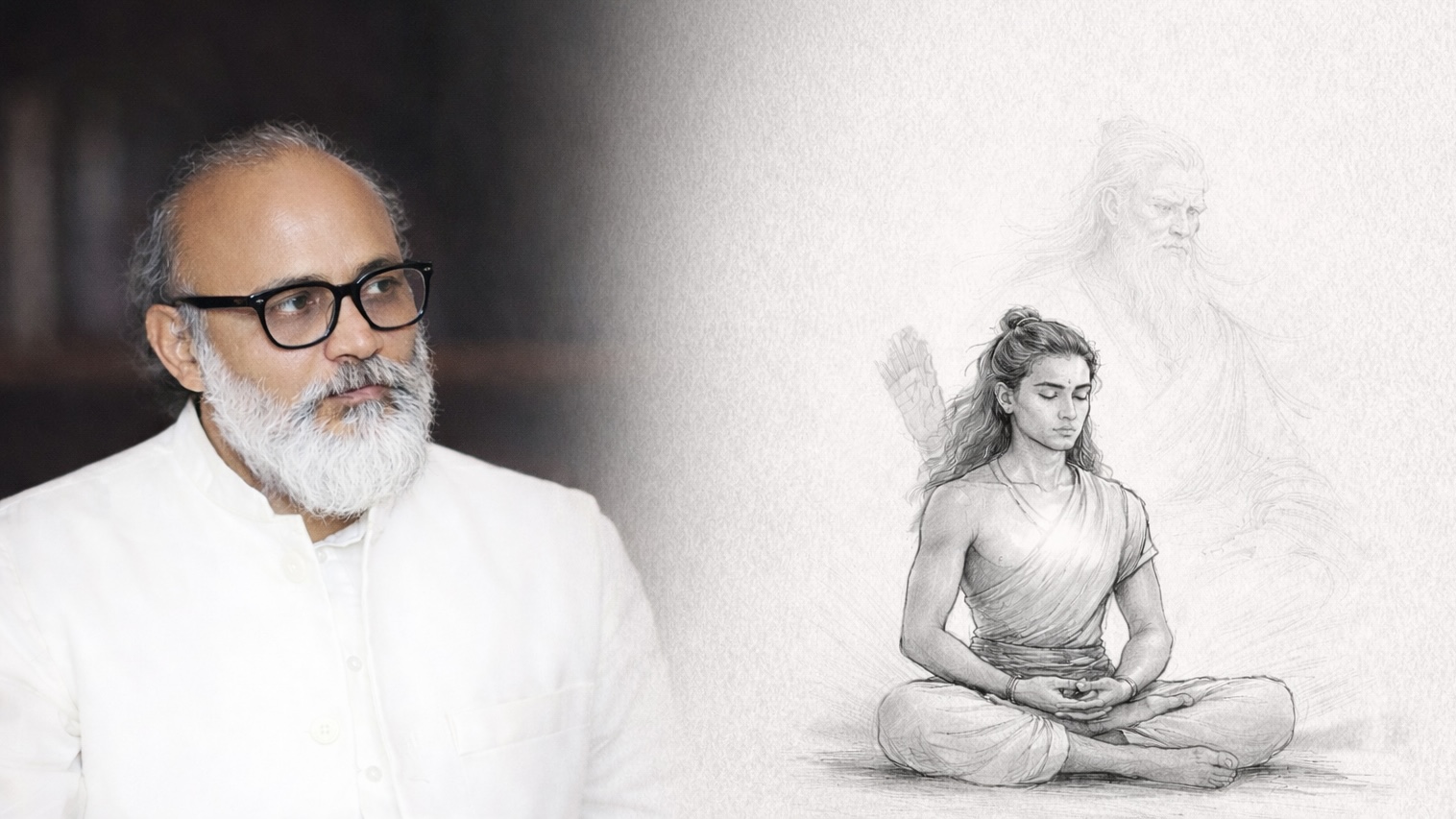
विद्या का चुराया जाना असंभव है
1 day ago By Yogi Anoopविद्या का चुराया जाना असंभव है
विद्या कोई वस्तु नहीं है जिसे छीना या चुराया जा सके। वह तो मनुष्य के अंतर्तम में छिपी हुई एक संभावना है, जो उपयुक्त स्थिति मिलने पर प्रकट हो जाती है। द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य से अंगूठा माँगे जाने की कथा को यदि केवल घटना के रूप में देखा जाए, तो वह अन्याय प्रतीत होती है; किंतु यदि उसे मानसिक वृत्तियों के स्तर पर देखा जाए, तो वहाँ एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई दिखाई देती है।
द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपना परम शिष्य माना था। उन्होंने यह भी घोषित किया था कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति ने किसी को इतना अधिक मान लिया हो, तो उस मान्यता को टूटते हुए देख पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। एकलव्य का कौशल केवल धनुर्विद्या में दक्षता नहीं था, वह द्रोण की उस धारणा के लिए चुनौती था, जिसे उन्होंने स्वयं निर्मित किया था। इसलिए वहाँ विद्या के चुराए जाने का प्रश्न नहीं था, बल्कि उस छवि के टूटने का भय था जिसे द्रोण ने अपने भीतर गढ़ लिया था।
जब हम किसी व्यक्ति, विचार या सिद्धांत को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दे देते हैं, तो उसे सही सिद्ध करने के लिए हम तर्क भी गढ़ते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतार्किकता का भी सहारा लेते हैं। जैसे तुलसीदास जी के लिए राम केवल राजा नहीं थे, वे भगवान थे। इस भाव को अक्षुण्ण रखने के लिए बलि को छिपकर मारने की घटना को भी पूर्वजन्म के कर्मों से जोड़ दिया गया। यहाँ सत्य की खोज नहीं, बल्कि आस्था की रक्षा अधिक प्रधान हो जाती है।
कर्म की अवधारणा भी यदि केवल बाहरी घटनाओं के स्तर पर देखी जाए, तो वह कभी समाप्त न होने वाला चक्र बन जाती है। मारने और मरने की श्रृंखला, प्रतिशोध और प्रतिफल का अंतहीन क्रम। यदि मुक्ति भी अगले कर्म पर निर्भर हो, तो फिर मुक्ति कहाँ है? यह प्रश्न हमें इस ओर संकेत करता है कि कर्म का समाधान कर्म में नहीं, बल्कि दृष्टि के परिवर्तन में है।
द्रोणाचार्य की कथा हमें यही सिखाती है कि जिसे हम अत्यधिक मान देते हैं, उसे बनाए रखने के लिए हम दूसरों के साथ अन्याय भी सहजता से कर बैठते हैं—और फिर उसे धर्म, मर्यादा या नियम का नाम दे देते हैं।
अपने अनुभव से मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि विद्या न तो दी जा सकती है और न ही छीनी जा सकती है। यदि किसी के भीतर विद्या का बीज ही नहीं है, तो कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई अभ्यास उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। और यदि वह बीज भीतर विद्यमान है, तो उसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। एकलव्य की विद्या उसकी अपनी थी। उसने केवल एकाग्रता के लिए द्रोण के चित्र को माध्यम बनाया, क्योंकि उस काल में द्रोण विद्या के प्रतीक बन चुके थे।
इससे यह भी समझ में आता है कि जो वस्तु हमसे दूर होती है, वह हमें अत्यंत श्रेष्ठ प्रतीत हो सकती है; पर निकट आने पर वही वस्तु अपनी सीमाएँ भी प्रकट कर देती है। इसलिए आकर्षण और सत्य को एक मान लेना स्वयं को भ्रम में डालना है।
विद्या बाहर नहीं है। वह भीतर है। और जो भीतर है, उसे न कोई चुरा सकता है, न छीन सकता है।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy