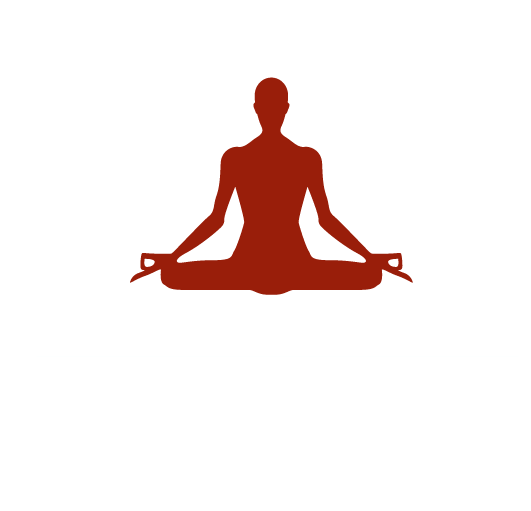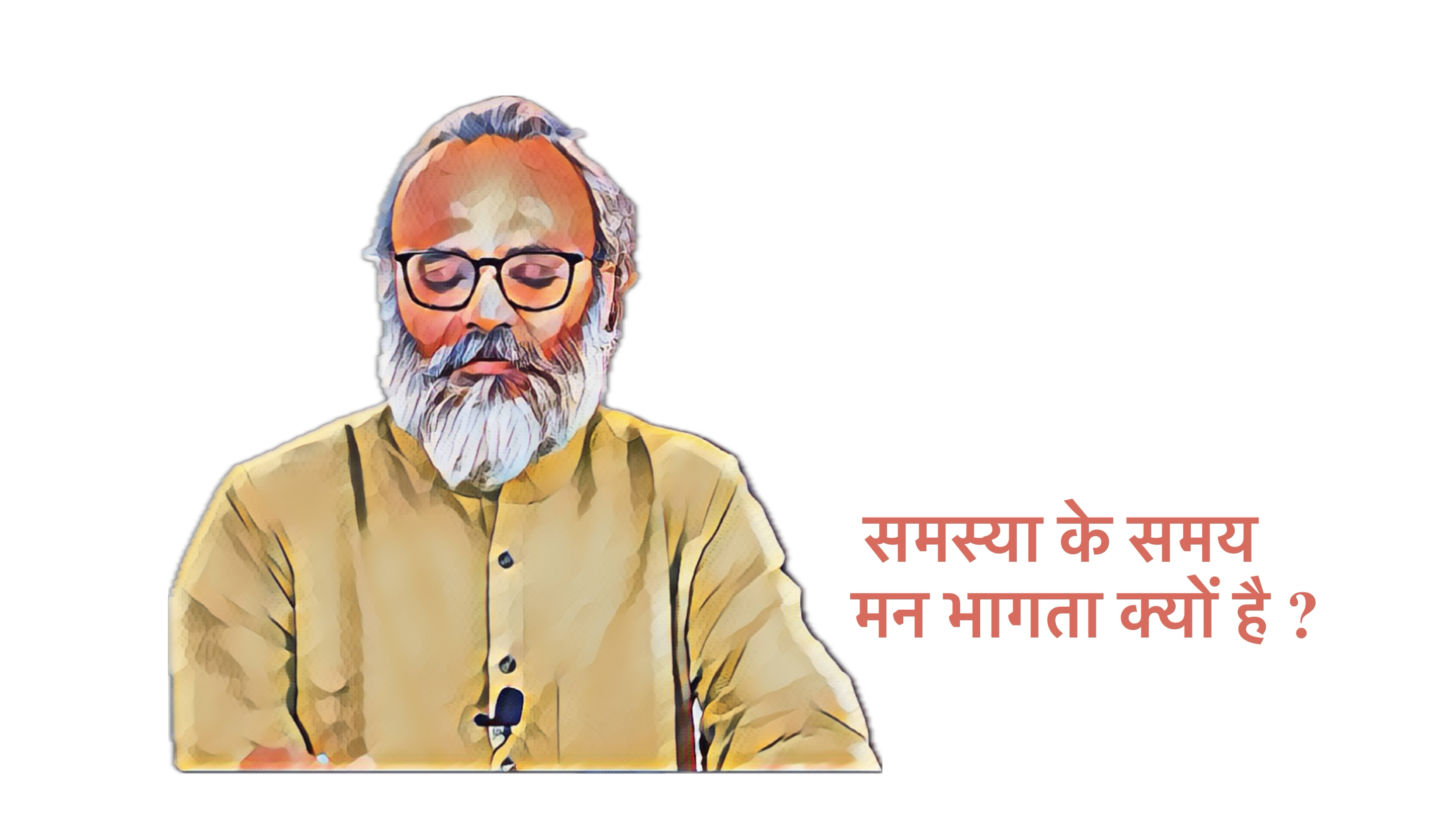
समस्या के समय मन भागता क्यों है ?
2 years ago By Yogi Anoopसमस्या के समय मन भागता क्यों है ?
यद्यपि मन के मूल स्वभाव के दो पहलू हैं, प्रथम स्थिरता और द्वितीय अस्थिरता । कुछ वैसे ही जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ।
यहाँ पर मन की अस्थिरता का तत्पर्य चलायमान होने से है । संसार को समझने के लिए उसे चलायमान होना पड़ता है । जब मन चलायमान होता है तभी उससे दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जब मन स्थिर होता है तब मनो शांति प्राप्त होती है । क्योंकि उस समय और काल में मन शांत व पंगुरहित हो गया ।
अब प्रश्न का समाधान करते हैं कि मन समस्या के समय बहुत तीव्र गति से चलने क्यों लगता है । यद्यपि समस्या के वक्त उसे चलना चाहिए क्योंकि समाधान मन को रोक देने से नहीं होगा । प्रश्न में मन के भागने का मूल तत्पर्य से है कि वह आवश्यकता से अधिक गति से भागने लगता है जिसके कारण उसमें समझने व सूझ बूझ की कमी दिखने लगती है ।
समस्या के समय मन इसलिए भागता है क्योंकि समस्या जब नहीं थी तब मन को कल्पनाओं में उड़ाने का प्रशिक्षण हमने पहले ही दे रखा है । पूर्व में यहाँ तक कि बचपन से ही मन कल्पनाओं को करके आराम पा रहा था । यदि कोई भी व्यक्ति अपने २४ घंटे में सोने के अतिरिक्त सभी समय को गौर से देखे तो यही मिलेगा कि उसका मन पूरे जागृत काल के समय क्षण-क्षण में कल्पनाओं के माध्यम से ख़ुशियाँ प्राप्त कर रहा होता है । यहाँ तक कि धार्मिक और भावुक क़िस्म का मन भी कल्पनाओं के माध्यम से भावनाओं को पैदा करके ख़ुशियाँ अंदर ले रहा होता है । यद्यपि वह उसे आनंद कहता है किंतु मैं उसे सिर्फ़ मनोकल्पित क्षणिक सुख ही कहता हूँ । समस्या यह है कि मन को प्रत्येक क्षण कल्पनाओं और भावनाओं से ख़ुशियों के प्राप्त करते रहने की बुरी आदत पड़ जाती है ।
यहाँ तक कि व्यवहार के समय भी उसका मन व्यवहार में न लगकर काल्पनिक भावनाओं में ओत प्रोत रहता है ।
यहाँ पर ध्यान देना आवश्यक है कि मन की लत कल्पनाओं में लग चुकी है । उसकी आदत व्यवहार में जीने की नहीं है । यहाँ तक कि व्यवहार में जीते हुए भी कल्पनाओं से आनंद प्राप्त करता रहता है ।
जैसे -ट्रक चलाते समय, ड्राइवर चलाने से अर्थात् अपनी स्किल से ख़ुशियाँ ना लेकर फूहड़ गानों से ख़ुशियाँ ले रहा होता है । जब कि उसे अपनी ड्राइविंग स्किल से ख़ुशियाँ लेना चाहिए था ।
यदि ध्यान से देखा जाये तो व्यवहार में मन को अधिक समय तक विश्राम मिलता है ।
जैसे भोजन का अधिकतम स्वाद लो तो कुछ घंटों तक भोजन की तरफ़ देखने तक का मन नहीं करता है । वह इसलिए कि मन संतुष्ट हो चुका है । यदि भोजन बिना स्वाद के सिर्फ़ पेट में भर लिया गया है तो असंतुष्ट मन का भोजन के प्रति आकर्षण जाता नहीं है । मन असंतुष्ट रहता है और यही कारण है कि उसका ध्यान भोजन के प्रति हमेशा रहता है ।
ध्यान दें वर्तमान में जब पूरी तरह से जीने का प्रयत्न किया जाता है तब गहन अनुभव होता है । और वही अनुभव मन को स्थिर कर देता है । मैं कहता हूँ कि अनुभव के भार से ही मन का भागना बंद हो सकता है अन्य किसी से नहीं ।
और ऐसे अनुभवियों को जब समस्या आती है तब उनका मन बहुत भागने के बजाय समाधान में लग जाता है । समाधान में मन को कल्पनाओं की उड़ान के बजाय बुद्धि व विवेक जैसों का अनुभवी साथ मिलता है । ध्यान दें समाधान की प्रक्रिया में भी मन को चलना पड़ता है पर अनुभव के साथ न कि कल्पनाओं में ।
ऐसे व्यावहारिक मन को समस्या का सामना करने के लिए भयभीत नहीं होना पड़ता है , यद्यपि उसमें शंकाओं का निर्माण हो सकता है किन्तु वह व्यावहारिक है । इसलिए क्योंकि उसने व्यवहार में मन को जीना सिखाया है ।
ध्यान दें समस्या व्यवहार में जीने में ही आती है और यदि मन व्यवहार में रहा ही नहीं तो उसे समस्या के दौरान भागने के अलावा और कुछ आएगा ही नहीं ।
जैसे भोजन करते समय मन का संलग्न होना पाचन और निष्कासन वाले सभी अंगों को स्वतः कार्य करना है । यदि भोजन करते समय भोजन से स्वाद ना निकाल कर आप कहीं और किसी कल्पित कल्पनाओं में स्वयं को व्यस्त किए हुए हैं तो आपका पाचन और निष्कासन वाले सभी अंग समस्या पैदा करेगा ।
अब जब वह समस्या पैदा करेगा तो गैस अधिक बनेगी , पेट फूलेगा , साँसे अटकना शुरू होगी तो अब आपका मन भागना शुरू करेगा । समस्या सामने खड़ी हो गई है , चूँकि आपने व्यवहार के समय या भोजन के समय भोजन के प्रति सतर्कता नहीं बरती , मन को भोजन से संतुष्ट करने के बजाय उसे भोजन करते समय कल्पनाओं से संतुष्ट करते रहे ।
कहने का मूल अर्थ है कि समस्या को हमने ही आमंत्रित किया , और आमंत्रित करके अब भाग रहे हैं । क्योंकि मन को व्यवहार में जीने की आदत लगभग ख़त्म हो गई है । यदि व्यवहार में उसने जिया नहीं तो व्यवहार में आने वाली समस्या का समाधान कैसे कर लेगा । अंततः वह किसी और से समाधान की आशा करेगा ।
यद्यपि वह यही तो पहले से करता ही आया था । वह तो इसी का अभ्यस्त है ।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy