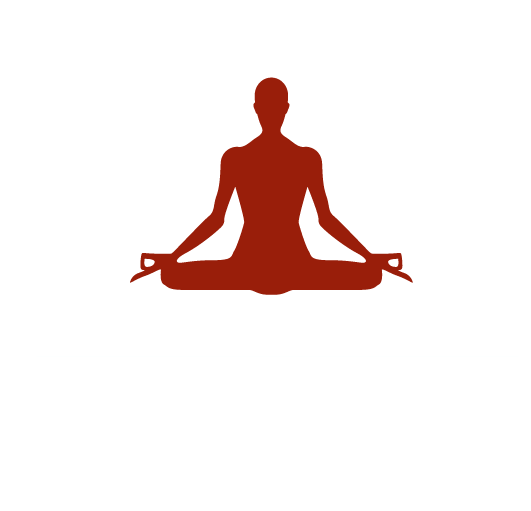शब्दों में स्थिरता से रोग
1 year ago By Yogi Anoopशब्दों में स्थिरता की भूल और वास्तविक जीवन की व्यावहारिकता
वर्तमान में हो रही घटनाओं का दोहराव असंभव है, क्योंकि हर पल परिवर्तन होता रहता है। जैसे लगता है कि हम नदी के एक ही जल में स्नान कर रहे हैं, लेकिन एक क्षण बाद देखें, तो उसी प्रवाह में से कितना जल निकल चुका होता है। इससे सिद्ध है कि एक जल में स्नान करना असंभव है । किंतु व्यक्ति स्वभावगत परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता है । उसे ऐसा आभास होता है कि परिवर्तन को देखते देखते स्वयं भी परिवर्तित होने लगता है । संभवतः इसीलिए व्यक्ति की लालसा होती है कि वह किसी स्थिर वस्तु या आधार को पकड़ ले, ताकि उसमें स्थिरता आ सके। स्थिरता का बोध हो सके ।
संभवतः इसी कारण कुछ गुरु परंपराओं में शब्दों को स्थिरता का आधार बनाया गया। उन्हें लगा कि यदि ध्यान को शब्दों पर एकाग्र किया जाए तो चित्त शांत और स्थिर हो जाएगा। यह विचार कुछ सीमा तक, विशेषकर पढ़ाई के समय, उचित भी था, जहाँ शब्दों पर टिकना महत्वपूर्ण माना जाता है।
लेकिन उम्र के एक पड़ाव के बाद, जैसे विवाह और व्यावसायिक जीवन में प्रवेश करने के बाद, शब्दों को स्थिरता का आधार बनाना एक भूल हो सकता है। इस काल में अत्यधिक व्यावहारिकता की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी इन्द्रियों का संपूर्ण उपयोग आवश्यक होता है।
मैंने ऐसे बच्चों और युवाओं पर भी अध्ययन किया है, जो शब्दों को पकड़ने में अत्यधिक अभ्यस्त होते हैं और परिणामस्वरूप व्यावहारिकता से दूर हो जाते हैं। उनमें अवसाद के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं क्योंकि शब्दों में जीने की आदत उनकी व्यवहारिकता में बाधा बन जाती है। जैसे किसी फल के स्वाद को केवल शब्दों में बताना असंभव है; स्वाद का असली बोध करने के लिए उसे चखना आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शब्दों में जीना संभव नहीं है, क्योंकि शब्द तो अपने आप उड़ जाते हैं। वे अनुभव की अनुभूति का आभास जरूर देते हैं, लेकिन वह वास्तविक नहीं होता।
इसी विचारधारा के आधार पर कुछ गुरु परंपराओं में शिष्यों को मंत्रों के अभ्यास पर बल दिया गया। कुछ परंपराओं में दैनिक क्रियाओं के दौरान मंत्रों के मानसिक उच्चारण की सलाह दी जाती है।
अगर दैनिक जीवन में अन्य कार्य करते समय बार-बार किसी मंत्र का मानसिक उच्चारण किया जाए, तो इसका अर्थ है कि हम एक समय में दो कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क कुछ वर्षों में थक जाता है और शरीर में कई रोग उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे जीवन का अर्थ व्यर्थ लगने लगता है।
यह मानना गलत होगा कि मंत्र सिद्धांत अर्थहीन है। मेरे अनुभव में, यह आत्मबोध का एक सशक्त साधन है, किंतु इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ध्यान दें कि मंत्र का उद्देश्य शब्दातीत अवस्था प्राप्त करना है, न कि प्रतिपल शब्दों का उच्चारण करना।
मंत्र सिद्धांत के अनुपालन के लिए कुछ सुझाव:
- मंत्र का उच्चारण विशेष समय, स्थान और परिधान में ही करें। ऐसा करने से मंत्र की सार्थकता अनुभव में आएगी; अन्यथा यह केवल मानसिक क्रिया बनकर रह जाएगी।
- मंत्रोच्चारण में शीघ्रता न करें। दो शब्दों के बीच उचित दूरी रखें और फिर शब्दों को तोड़कर अक्षरों में भी उचित दूरी का प्रयास करें। ऐसा करने से मंत्र शब्दातीत अवस्था की ओर ले जाते हैं, अर्थात निःशब्दता को प्राप्त करते हैं।
- दो शब्दों के बीच की शून्यता का अनुभव करें। इस शून्यता का अनुभव हमें निष्क्रिय अवस्था में स्थिर रहने की आदत डालता है, जिससे शून्यता में प्रवेश की प्रेरणा मिलती है। जब अभ्यासी इस शून्यता पर ध्यान केंद्रित करता है, तो आत्मअनुभूति के संकेत स्वतः मिलने लगते हैं।
- मंत्र को साधन बनाएं, लक्ष्य नहीं। मंत्र केवल माध्यम है, स्वयं की अनुभूति का प्रयास करना ही असली उद्देश्य है।
इस प्रकार, मंत्र सिद्धांत का अभ्यास हमें निःशब्द अवस्था और आत्मबोध की ओर ले जाने में सहायक होता है।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy