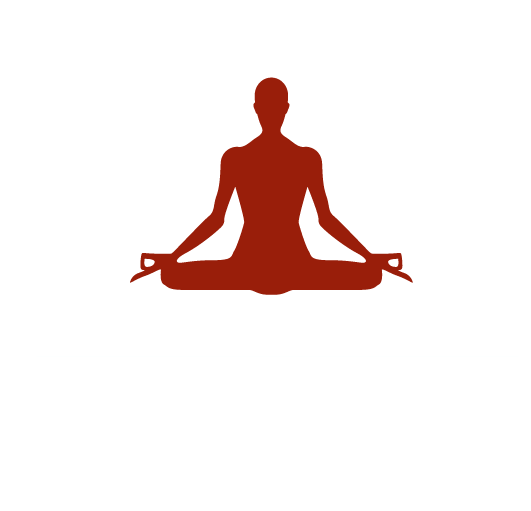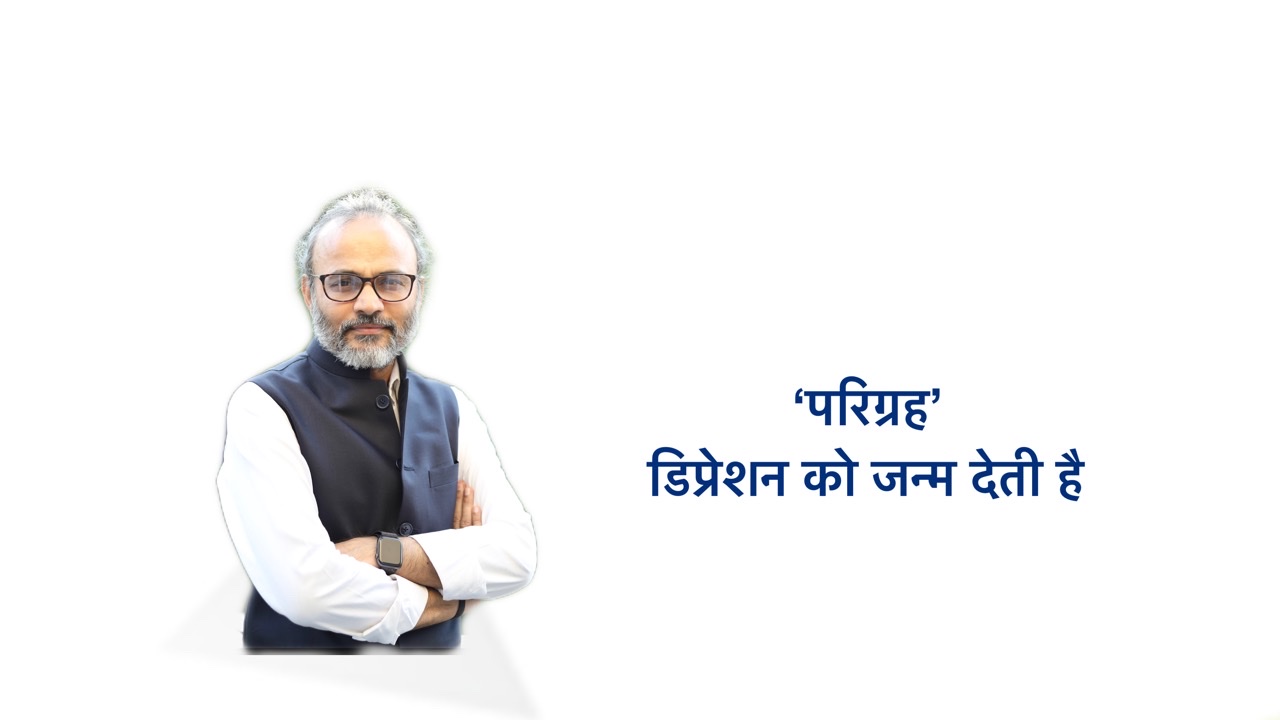
‘परिग्रह’ डिप्रेशन को जन्म देती है
3 years ago By Yogi Anoop‘परिग्रह’ डिप्रेशन को जन्म देती है
भारतीय दर्शनिकों एवं ऋषियों ने अपरिग्रह पर हमेशा महत्व दिया । उनका कहना था कि विचारों और भावनाओं का जितना अधिक से अधिक परिग्रहण होता जाएगा उतना अवसाद व डिप्रेशन बढ़ता जाएगा और साथ साथ चित्त का घड़ा भी भरता जाता है । जीवन में एक समय सीमा के बाद भारतीय परम्पराओं में अपरिग्रह के अभ्यास पर ज़ोर दिया गया । उनका कहना था कि भावनाओं और विचारों का परिग्रह मस्तिष्क की क्षति करने लगता है, वह इसलिए क्योंकि अंतरतम में भावनाओं का भराव आवश्यकता से अधिक हो जाता है , जिसके कारण वे आपस में ही लड़ने लगती हैं , और उस लड़ने कारण स्वसंतोष लगभग समाप्त हो जाता है । इसलिए उन भावनाओं को जो स्वयं को भारी बनाए हुए हैं, उसे बाहर निकाल फेंकना भी आवश्यक भी आवश्यक होता है ।
एक उदाहरण से इसे और समझने का प्रयत्न का चाहिए -
किसी घर में वर्षों वर्षों तक वस्तुओं को इकट्ठा करते रहने पर घर के अंदर स्थान की कमी महसूस होने लगती है । रहने वाले व्यक्ति को घुटन महसूस होनी शुरू होती है । प्रमुख कारण है कि वस्तुओं के भराव की अति हो रही है , वस्तुओं ने आवश्यकता से अधिक स्थान को घेर कर रखा हुआ है , परिणाम यह होता है कि कुछ वर्षों के बाद रहने वाले के लिए भी स्थान की कमी महसूस होनी शुरू हो जाती है ।
बिलकुल उसी प्रकार विचारों और भावनाओं को वर्षों वर्ष तक परिग्रह व इकट्ठा करते रहने पर उसमें रहने वाले को घुटन महसूस होनी प्रारम्भ हो जाती है । उन विचारों और भावनाओं में इतनी अधिक चुम्बकीय शक्ति जागृत कर दी गयी है कि उससे व्यक्ति परेशान हो उठता है । उसको लगता है कि ये उससे अधिक शक्तिशाली हैं , उन्हें ऐसा मिथ्याभाश होने लगता है कि इन आदतों को समाप्त नहीं किया जा सकता है । यही कारण है कि उसे किसी दूसरे का सहयोग लेने का मन करता है । स्वयं में असहाय होने पर वह कर भी क्या सकता है क्योंकि उसे स्वयं के मस्तिष्क और देह में ही अकेलापन लगने लगता है , ऐसा लगता है कि साँसों की कमी हो रही है , न व्यक्त कर पाने वाली उलझने शुरू हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि वह स्वयं से ऊब गया है । अंततः जीवन निरर्थक हो जाता है ।
कहने का मूल अर्थ है कि अज्ञानतावश वह स्वयं के बनाए हुए जाल में फँस गया होता है । उससे निकलने के लिए वह और परिग्रहण का जाल बुनता है किंतु समस्याएँ कम होने के बजाय विकराल होती जाती है ।
ध्यान दें जो समस्या परिग्रह से हो रही हो उसके समाधान में और परिग्रह भला कैसे उचित रहेगा । यह तो कुछ ऐसा ही समाधान है जैसे एक कमरे में वस्तुओं की संख्या अधिक हो गयी है और हम है कि बजाय कि वस्तुओं को बाहर फेकने के उस कमरे में कुछ और वस्तुओं को भर रहे होते हैं । ये समस्या का समाधान नहीं है बल्कि समस्या को और भयावह करना है ।
अग्नि का शमन अग्नि से नहीं बल्कि उसके विपरीत गुण वाले पानी से ही होता है । बिलकुल उसी प्रकार जो दुःख व अवसाद परिग्रह से उत्पन्न हो रहा हो उसके निराकरण के लिए कुछ और shopping करना मूर्खता है । उसे तो अपरिग्रह का ही पालन करना होगा । और यदि नहीं कर पाता तो अंत में उसे आधुनिक चिकित्सीय प्रणाली की झोली में गिरना ही पड़ता है । और वह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें देह के किसी एक अंग को ठीक करने की चेष्टा में अन्य दूसरे अंगों का भी बेड़ाग़र्क हो जाता है ।
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह ज्ञात हो जाता है कि परिग्रहण के इस चक्कर मे उसकी उलझने और बढती जाती हैं । इसीलिए भारतीय मनीषियों ने अपरिग्रह को जीवन का आधार बनाया , इसे आध्यात्मिक ही नहीं भौतिक जगत में शांति का आधार बताया ।
वस्तुओं का संग्रह ही नहीं बल्कि भावनाओं के संग्रह पर ध्यान रहे । यह सब आवश्यकनुसार ही होनी चाहिए , आवश्यकता की पूर्ति के बाद उसे त्यागने में संकोच नहीं होनी चाहिए ।
भावनाओं का संग्रह अधिक ख़तरनाक है , उसे कम से कम करने के लिए ज्ञान आवश्यक है । किसी अनुभवी गुरु के संरक्षण में ध्यान का अभ्यास करें ।
रात्रि काल में विचारों और भावनाओं के संग्रह को कम से कम करें । स्क्रीन न देखें तो सर्वोत्तम है ।
रात्रि काल में भोजन की अति से बचें । भोजन के रव अपनी मांसपेशियों को ढीला करने का अभ्यास करें जिससे रात में भोजन पर अति निर्भरता समाप्त हो जाएगी ।
सोने के पूर्व बिस्तर पर योग निद्रा करते करते सो जाएँ । इससे विचारों, भावनाओं और मांसपेशियों को ढीला करने में सहायता मिलती है ।
उसी प्रकार का भोजन करें जिससे क़ब्ज़ न हो , मल त्याग भी आवश्यक है ।
दान अवश्य दें, यह न देखें कि वह उसका क्या करेगा, यह देखें कि आपको शांति मिले ।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy