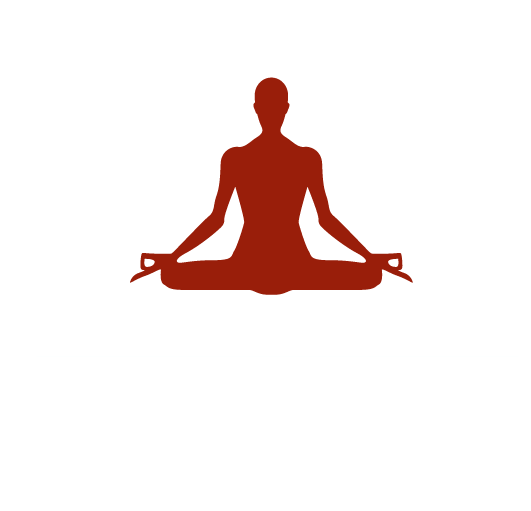प्राणायाम: मन पर अनुशासन
11 months ago By Yogi Anoopप्राणायाम; मन को अनुशासित करने का एक माध्यम है
योग साधना में प्राणायाम मात्र श्वास-प्रश्वास की गति का अभ्यास नहीं, अपितु श्वास के माध्यम से मन को अनुशासित करने की गूढ़ विधि है। यह केवल हवा का भीतर लेना और बाहर छोड़ना नहीं, बल्कि मन की गहराइयों में उतरने का विज्ञान है। जब साँसे लगातार तनाव में रहती हैं—अर्थात न भीतर जाने में विश्राम और न ही बाहर छोड़ने में सहजता—तो यह इस बात का संकेत है कि मन साँसों के अभ्यास के माध्यम से स्वयं को सतत अशांत और असंतुलित बनाये हुए है।
यदि मन को संतुलित करना है तो कम से कम किसी एक दिशा में उसे विश्राम का अवसर देना होगा। श्रम और विश्राम, ये दोनों अवस्थाएँ प्रकृति के सहज नियम हैं। जैसे परिश्रम के पश्चात विश्राम आता है और विश्राम के बाद पुनः कर्मशीलता जागृत होती है। जब इस प्राकृतिक लय को समझ लिया जाए, तभी प्राणायाम के वास्तविक रहस्य का बोध संभव हो पाता है।
श्रम और विश्राम का गूढ़ विज्ञान
गहरी निद्रा की अवस्था में शरीर और मन दोनों पूर्णतः विश्राम में होते हैं। उस समय समस्त तंत्रिकाएँ और मानसिक तरंगें शांत हो जाती हैं। यह विश्राम अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इसके बिना मनुष्य की चेतना स्थिर नहीं रह सकती। परंतु ध्यान दीजिए, यह शांति स्थायी नहीं होती। कुछ समय पश्चात शरीर के अंतःतंत्र स्वयं को पुनः सक्रिय कर देते हैं। तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जिससे इंद्रियाँ पुनः जाग्रत हो जाती हैं और संपूर्ण शरीर क्रियाशील हो उठता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोर्टिसोल हार्मोन्स के स्राव के कारण जागृति नहीं होती बल्कि सम्पूर्ण तंत्र के स्वभाव में विश्राम और श्रम छिपा हुआ है , उस जागृति व परिश्रम वाले स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न हार्मोन्स (कार्टिसोंल और सेरोटोनिन मेलाटोनिन ) का स्राव होता है । स्वभाव पहले आता है ।
ध्यान दें यह जागरण भी उतना ही आवश्यक है जितना विश्राम। यदि मनुष्य केवल सोता ही रहे तो जीवन संभव नहीं, और यदि विश्राम न मिले तो शरीर व मन दुर्बल होकर विकारग्रस्त हो जाएगा । यह निरंतर परिवर्तनशील चक्र—श्रम और विश्राम, जागरण और निद्रा—प्राकृतिक सृष्टि की सर्वाधिक अद्भुत व्यवस्थाओं में से एक है।
गूढ़ अनुभूति: संतुलन ही आत्मबोध का द्वार
सिद्ध गुरु योगी अनूप जी के अनुसार, प्राणायाम का लक्ष्य केवल श्वास को लयबद्ध करना नहीं, बल्कि इन साँसों के माध्यम से मन स्वयं को विश्राम और श्रम करने को प्रशिक्षित करता है । और चेतना के प्रवाह को नियंत्रित कर उसे विश्राम और श्रम के मध्य सम्यक संतुलन में स्थापित करना है। जब साधक इस संतुलन को साधने में समर्थ हो जाता है, तब उसकी चेतना में एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। वह केवल बाहरी संसार की हलचल से मुक्त नहीं होता, बल्कि अपने आंतरिक स्वरूप का भी साक्षात्कार करने लगता है।
यदि यह संतुलन न बना रहे तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, यदि कोई सोने के बाद जाग ही न पाए! या फिर दिन-रात जागता ही रहे और विश्राम का अवसर न मिले! यह प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है कि हम हर दिन सोते हैं, फिर जागते हैं और पुनः सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु यह चक्र स्वाभाविक रूप से उन्हीं के लिए सहज है जो अपनी चेतना को संतुलित रखना जानते हैं।
प्राणायाम: आत्मबोध का प्रवेशद्वार
प्राणायाम का गूढ़ उद्देश्य केवल श्वास को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि मन और चित्त-वृत्तियों को संतुलित करना है। जब साधक अपनी श्वास को सहजता से साध लेता है, तो मन अपने आप उस गहराई में उतरने लगता है . इसे इस प्रकार समझना और अधिक बेहतर होगा कि मन प्राणायाम के माध्यम से स्वयं को साधता है । अर्थात प्राणायाम एक माध्यम है मन को प्रशिक्षित करने का ।
जब मन प्राणायाम के माध्यम से विश्राम करना सीखने लगता है तब देह तंत्र पर दुष्प्रभाव बंद हो जाता है , या यूँ कहें कि कम से कम हो जाता है और देह स्वयं को स्वयं के द्वारा ही हील कर लेती है ।
जहाँ विचारों की चंचलता समाप्त हो जाती है और आत्मबोध का प्रकाश प्रस्फुटित होता है। यही संतुलन योग का वास्तविक आधार है, और यही आत्मज्ञान की प्रथम सीढ़ी भी।
योगी अनूप जी के अनुभव के अनुसार, प्राणायाम की सफलता केवल तकनीकी अभ्यास में नहीं कि फेफड़े को कितना शक्तिशाली बना दिया गया है , अपितु इसके पीछे मन को प्रशिक्षित करने से है । ध्यान दें मन का किसी भी अंग पर आवश्यकता से अधिक ध्यान केंद्रित करना भयानक हो सकता है इसीलिए मन को अंगों से कुछ काल के लिए स्वतंत्र कराया जाता है ।
इसलिए इसमें आंतरिक अनुभूति और मनोवैज्ञानिक संतुलन निहित होना चाहिए । जब साधक अपने मन और श्वास को एक ही लय में प्रवाहित करना सीख लेता है, तब वह केवल बाहरी संसार से ही नहीं, स्वयं के भीतर की हलचलों से भी मुक्त हो जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ साधक स्वयं को वास्तविक रूप में अनुभव करता है—अजन्मा, अजर, और अविनाशी।
अतः, प्राणायाम को केवल एक शारीरिक क्रिया के रूप में देखना इसकी सीमाओं को सीमित करना होगा। यह केवल श्वास का नहीं, अपितु आत्मा के परम बोध का साधन है। जब साधक इसे पूर्ण निष्ठा से अपनाता है, तभी वह अपने भीतर उस चेतना को जाग्रत कर सकता है जो सदा से विद्यमान थी, परंतु अब तक सुप्त अवस्था में थी। यही प्राणायाम की सिद्धि है, और यही आत्मबोध का आरंभ भी।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy