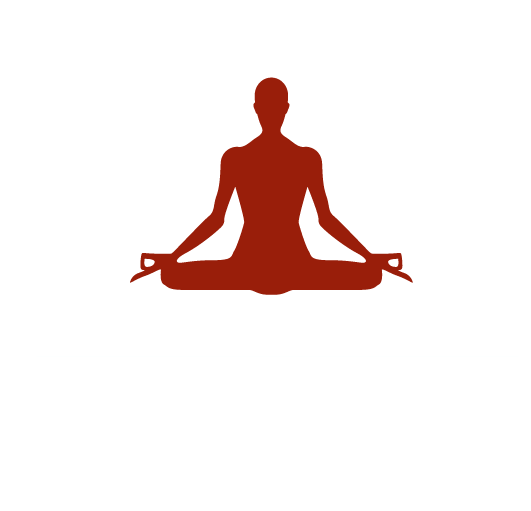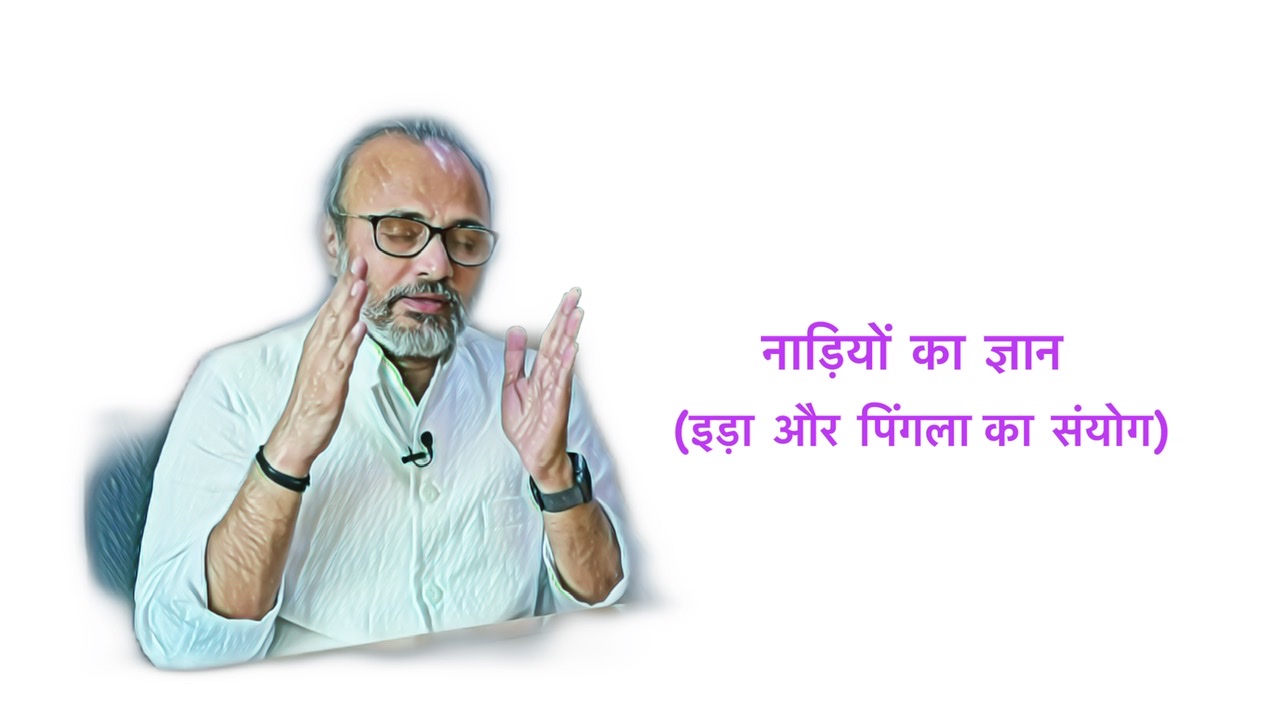
नाड़ियों का ज्ञान
3 years ago By Yogi Anoopनाड़ियों का ज्ञान
सामान्यतः नाड़ियों को नसों से सम्बद्ध कर लिए जाता है, सभी को ऐसा लगता है कि नाड़ियाँ और नसों में कोई अंतर नहीं है । किंतु यौगिक दृष्टिकोण से इनके मध्य बहुत बड़ा अंतर होता है । जैसे प्रत्येक डेढ़ से दो घंटों में दोनों नासिका में से किसी एक में साँसों की गति थोड़ा सा कम हो जाती है और दूसरे में अधिकता हो जाती है । यही प्रक्रिया डेढ़ से दो घंटे में बदल जाती है । बहुत कम ऐसे समय देखा जाता है जिसमें दोनों नासिका में बराबर मात्रा में साँसों का आवागमन होता रहता है ।
जिस नासिका से साँसों का आवागमन कम हो जाता है, इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि उस नाक का रास्ता सिकुड़ गया । उस नासिका में साँस के आने जाने में कोई अवरोध नहीं है , कोई बाधा नहीं होती है किंतु फिर भी किसी एक नासिका के अंदर से साँसों के आवागमन कमी हो जाता है । और कुछ घंटों के बाद में वही नासिका साँसों को अधिक तेज़ी से लेने और छोड़ने लगती है और दूसरी नासिका के अंदर साँसों के अंदर अवरोध शुरू हो जाता है ।
इन साँसो की प्रक्रिया में जो नाक तेज चल रही होती है, कुछ ही घंटों में बाधित होने होने लगती है । इसके बाधित होने का मूल करण नाक के अंदर नसों का सिकुड़न नहीं बल्कि नाड़ियों के करण होता है ।
इसी प्रक्रिया को ही हम नाड़ी कहते हैं । यह दृश्य में नहीं है , इसे नसों व हड्डियों की तरह देखा नहीं जा सकता है किंतु इसे स्वयं के नाक में साँसों की प्रक्रिया के माध्यम से समझा जा सकता है ।
इसी को ध्यान में रखते हुए हठ योगियों ने इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का नाम दिया । जो वास्तव में शरीर की प्रत्येक गतिविधियों को सूक्षतम रूप से नियंत्रित करता है । यह मस्तिष्क से और मस्तिष्क स्वभाव से नियंत्रित होता है । इसीलिए राज योग में यम नियम के अभ्यास पर अधिक ज़ोर दिया गया । यद्यपि हठ योग में आसन प्राणायाम और एकाग्रता के माध्यम से इन नाड़ियों में तीव्रता लाने का अभ्यास करवाया जाता है ।
इसीलिए हठ योगियों ने उन्हीं आसनों और प्राणायाम के अभ्यास पर ही ज़ोर दिया जो उस व्यक्ति विशेष की कमजोर नाड़ी में तेज़ी ला सके जिससे उसका स्वभाव और बेहतर हो सके । हठ योगी कहता है नाड़ियों में बदलाव करके स्वभाव में उच्चतम अवस्था लाया जा सकता है और शरीर को स्वस्थ्य भी किया जा सकता है ।।
यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह नासिका तो सिर्फ़ बाह्य भाग है जिसे आसानी से अनुभव किया जा सकता है , ऐसे ही शरीर के बहुत सारे भाग होते हैं जो इसी प्रकार संचालित होते हैं । चूँकि देह में जल और वायु की सबसे अधिक निर्भरता होती है इसलिए नाक के अंदर इसे आसानी से अनुभव किया जा सकता है ।
यदि बहुत गम्भीरता से देखा जाए तो दोनों नाकों में एक के बाद एक नाक की बंद होने की प्रक्रिया मस्तिष्क के पैटर्न से संचालित होती है । मस्तिष्क का जो हिस्सा अधिक कार्यरत होता है वह उसके उल्टी दिशा में नाक अधिक तेज़ी से चलने लगती है ।
उदाहरण से इसे समझने में सहायता मिलेगी -
यदि बायाँ मस्तिष्क अधिक क्रियाशील हो गया तो दाहिनी नाक पूर्ण रूप स्वतः खुल जाती है और उसमें साँसे बहुत आसानी से अंदर और बाहर आने लगती हैं । साथ साथ दाहिनी नासिका के पूर्ण रूप से खुलते ही बायीं नासिका में अवरोध उत्पन्न होने लगता है । अर्थात् बायीं नासिका से साँसे लगभग चलनी बंद हो जाती हैं । इसी प्रकार बायीं नासिका के पूर्णतः खुलकर चलने से दाहिना मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है साथ साथ दाहिनी नाक को लगभग बंद कर देता है ।
यद्यपि दैनिक क्रियाओं को करते समय हम सभी नाड़ियों के इस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दे पाते हैं किंतु यह प्रक्रिया घटती सभी के साथ है ।
इस सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि मस्तिष्क के किसी एक हिस्से दाहिने व बाएँ के चलने पर नाक के अंदर चलने वाली साँसों पर प्रभाव पड़ता है । यदि और गहराई से सूक्ष्म रूप में अध्ययन किया जाए तो यह मस्तिष्क स्वभाव और शरीर की आवश्यकताओं से संचालित होता है । जैसे जैस सोचने और विचार करने की प्रक्रिया बढ़ती है वैसे वैसे नाड़ियों पर प्रभाव धटता बढ़ता रहता है ।
ये नाड़ियाँ शारीरिक आवश्यकतानुसार भी चलती हैं जैसे , भोजन करने के बाद दाहिनी नासिका स्वतः ही तीव्रता में चलने लगती है बायीं नासिका से साँसों का आवागमन बहुत कम व न के बराबर हो जाता है ।
और साथ जब व्यक्ति गहरी नींद में जा रहा होता है तब बायीं नासिका ही जागृत हो जाती है । बायीं नासिका का अर्थ इड़ा नाड़ी का क्रियाशील हो जाना ।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy