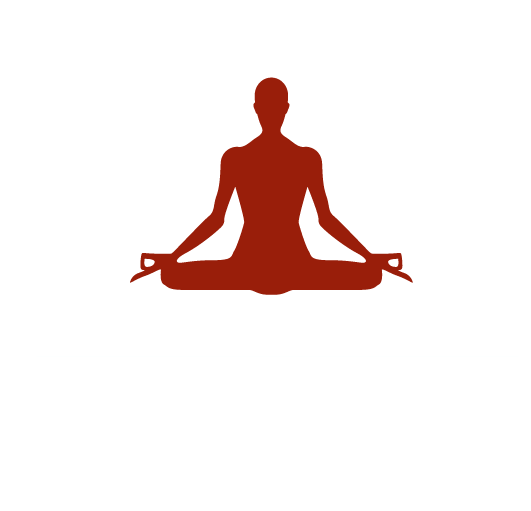कर्मयोग और एकाग्रता का गूढ़ विज्ञान
1 year ago By Yogi Anoopकर्मयोग और एकाग्रता का गूढ़ विज्ञान
एकाग्रता का स्तर दो प्रकार से बढ़ता हुआ अनुभव किया जा सकता है—प्रतिकूल परिस्थितियों और जोखिम लेने की प्रवृत्ति से। हालांकि अनुकूल परिस्थितियों में भी एकाग्रता बढ़ने की संभावना रहती है, परंतु उसमें सफलता लगभग न के बराबर होती है। इसका एक मुख्य कारण है—किसी एक भाव में बहने की आदत। ऐसी स्थिति में मन और विचारों को रोकने की क्षमता का अभाव दिखता है, जिससे मस्तिष्क के समस्त तंत्रों का समुचित विकास संभव नहीं हो पाता।
इसके विपरीत, प्रतिकूल परिस्थितियां और जोखिम लेने की प्रवृत्ति एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करती हैं, जिसमें एकाग्रता को मजबूरन बढ़ाना पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में विचारों के प्रबंधन की क्षमता का स्वतः ही विकास होता है। और यदि यह प्रक्रिया आध्यात्मिक प्रवृत्ति से जुड़ी हो, तो व्यक्ति निष्काम कर्मयोगी बन सकता है। इसे मैं मन और मस्तिष्क का पूर्ण विकास मानता हूँ।
भय, पराजय का डर, अस्तित्व पर संकट, और योजनाओं को क्रियान्वित करने की क्षमता — ये सभी ऐसी अवस्था में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। इस दौरान विचारों को रोकने की क्षमता का विकास भी करना पड़ता है। तथाकथित नकारात्मक विचारों से बचने के बजाय उनसे लड़ना आवश्यक हो जाता है। ध्यान देने पर समझ में आता है कि इस परिस्थिति में एकाग्रता का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। इस समय मन, इंद्रियां और दैहिक तंत्र प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने के लिए संगठित होकर कार्य करते हैं और व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं।
एक उदाहरण:
परिवार में किसी आपदा या दुखद घटना के समय, मन की एकाग्रता देखने योग्य होती है। उस समय मन, इंद्रियां और दैहिक तंत्र उस आपदा का समाधान खोजने में पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाते हैं। उस समय मन किसी कल्पना में व्यस्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एकाग्रता समस्या के समाधान में लगी होती है।
हालांकि जीवन में आपदाएं बार-बार नहीं आतीं, लेकिन समस्याएं तो रहती ही हैं। चाहे वे मानसिक हों, दैहिक हों, या बाहरी, उनके समाधान के लिए व्यक्ति अपनी एकाग्रता का विकास कर सकता है। आजकल बहुत से लोग एकाग्रता की कमी की शिकायत करते हैं। वे पूछते हैं, “मन कैसे एकाग्र हो?” यह भी एक प्रकार की साधना हो सकती है, किंतु इसमें तीव्र विकास की संभावना कम रहती है। अनुकूल परिस्थितियों में मन भागने के रास्ते आसानी से खोज लेता है। परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में, मन के भागने के मार्ग लगभग समाप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिकता के सहयोग से इन प्रतिकूल समयों में एकाग्रता को विकसित किया जा सकता है।
दूसरा उदाहरण:
मेरा एक शिष्य अक्सर पूछता है, “मृत्यु कैसे आएगी?” फिर कुछ दिनों बाद, “शरीर में झुर्रियां क्यों पड़ रही हैं?” और कभी, “मुझे हर समय भय महसूस होता है, इससे कैसे बचा जाए?” ऐसे हजारों प्रश्नों से वह स्वयं को घेर लेता है। लगभग हर दूसरा शिष्य इसी तरह के प्रश्न करता है। मेरा प्रयास रहता है कि उसे आत्म-प्रबंधन के माध्यम से सही मार्ग पर लाया जाए। कई बार मेरा मन उद्वेलित और क्रोधित हो उठता है, किंतु मैं स्वयं को नियंत्रित कर शिष्य को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ।
व्यावहारिक अनुभव:
मेरा अनुभव है कि बाहरी जगत में प्रबंधन जितना बढ़ता है, उतना ही मनो-जगत में भी प्रबंधन बढ़ता है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मैं मानता हूँ कि जीवन में छोटी-मोटी समस्याओं का आना-जाना आवश्यक है। इससे मन और दैहिक तंत्रों में प्रबंधन की क्षमता स्वतः विकसित होती है। व्यक्ति स्वयं पर कार्य करने में सक्षम बनता है। अन्यथा किसी एक भाव में रहने की आदत व्यक्ति का सर्वनाश कर देती है।
प्रतिकूल परिस्थितियों का महत्व:
जहां प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, वहां व्यक्ति को हर कदम फूंक-फूंक कर रखना पड़ता है। निर्णय अत्यंत सोच-समझकर लेने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में एकाग्रता और मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है। मस्तिष्क के सूक्ष्म हिस्से सक्रिय होकर निर्णय लेते हैं और स्थिरता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत, अनुकूल परिस्थितियों में इंद्रियों और मन का उच्च विकास संभव नहीं हो पाता। क्योंकि भावनाओं में बहने की प्रवृत्ति से विचारों की गति को रोकने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy