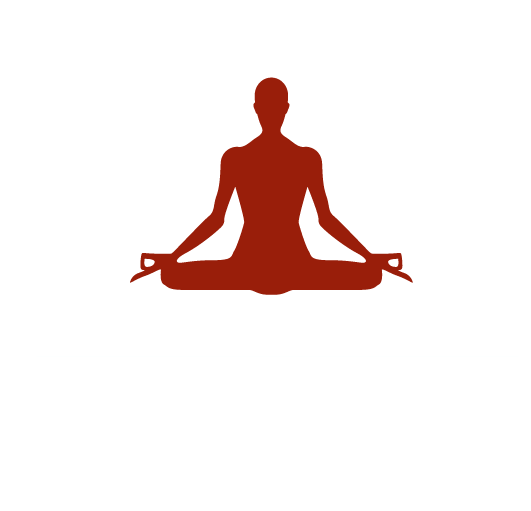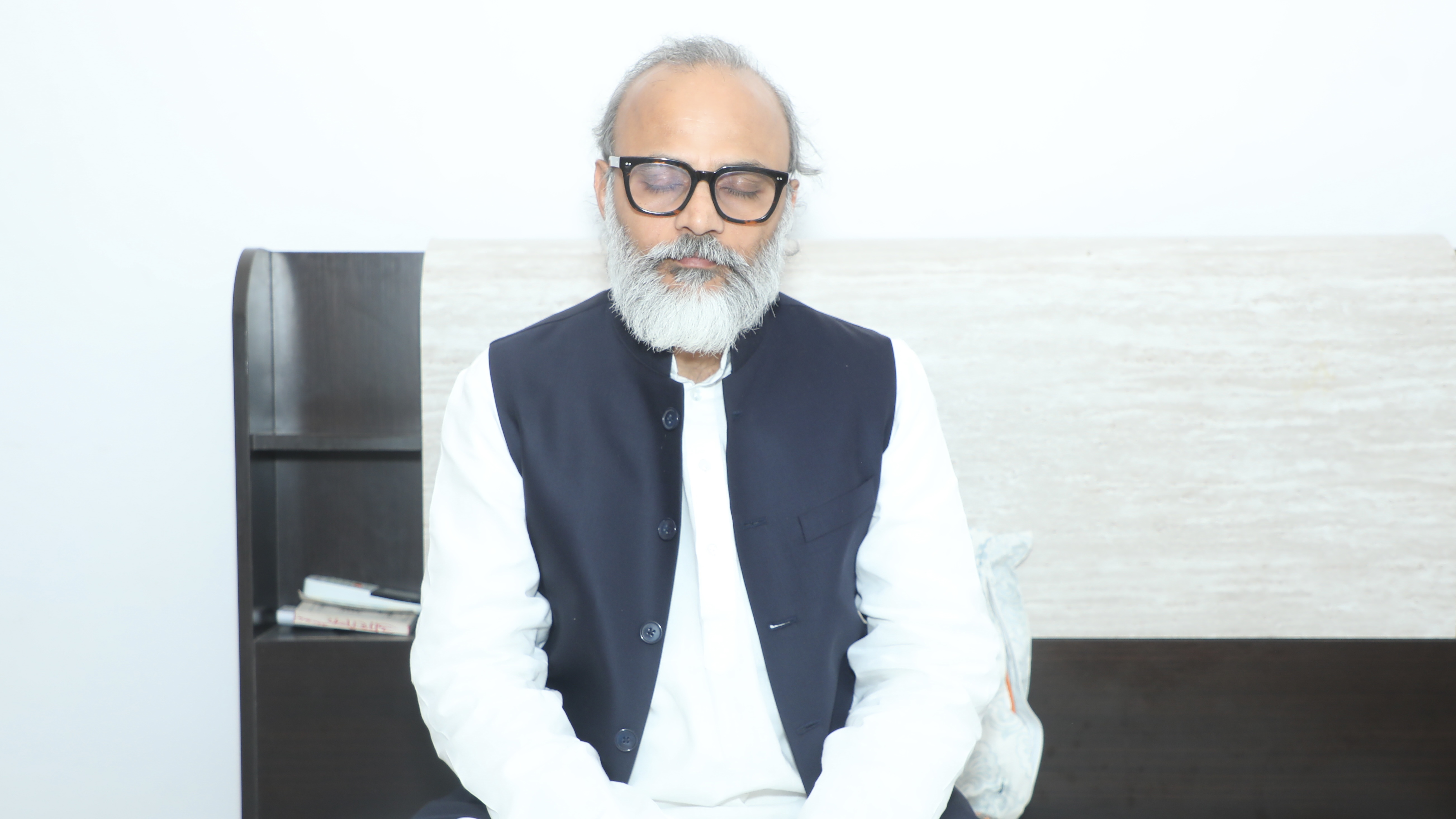
कल्पना की गति पर नियंत्रण
9 months ago By Yogi Anoopकल्पना की गति पर नियंत्रण: ध्यान का गूढ़ विज्ञान
ध्यान का सबसे गहरा पक्ष यह है कि मनुष्य अपने कल्पना की गति (Speed of Imagination) को नियंत्रित कर सके। साधारणतया, ध्यान का अर्थ विचारों का शून्य अवस्था से होता है । किंतु विचारों की गति और संख्या इतनी अधिक होती है कि उसे शूनावस्था में ले जा पाना संभव नहीं हो सकता है । बहुत तीव्र रफ़्तार में चलती हुई कार को छनक कैसे रोका जा सकता है ! यह असंभव प्रक्रिया होती है । इसीलिए मैं हमेशा कल्पनाओं और विचारों की तीव्र गाती को धीमे करने का प्रयत्न करवाता हूँ । उसके बाद रुकने की क्रिया संभव हो सकती है ।
यह सत्य है “मैं” ने मन के स्वभाव को चंचल होने में अभ्यस्त कर दिया है । आदतवश बिना किसी ठोस कारण के इधर-उधर भटकता रहता है। कुछ न कुछ निर्मित व निर्माण करने की अदालत के कारण कल्पनाएँ कभी अतीत की ओर दौड़ती हैं, कभी भविष्य की ओर। किंतु यह अनियंत्रित कल्पनाशीलता को मैं भटकना कहता हूँ । क्योंकि यह बिना किसी उद्देश्य के मन के द्वारा किसी न किसी कल्पना और विचारों का निर्माण किया जाता रहता है । अंततः यह मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट कर देती है, उसे मानसिक थकान, चिंता और अशांति की ओर ले जाती है।
जब हम ध्यान की बात करते हैं, तो उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि इस कल्पनाशक्ति को नियंत्रित किया जाए, इसे अनुशासित किया जाए, और इसकी गति को धीमा किया जाए।
मानव मन के समक्ष दो मार्ग होते हैं—
1. कल्पना को रोकने के बजाय उसकी गति को धीमा करना – जिससे व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में उतरकर मानसिक शांति प्राप्त कर सके।
2. कल्पना की गति को बढ़ाना – जिससे व्यक्ति विचारों के जाल में उलझकर अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को व्यर्थ गँवा दे।
अधिकांश लोग अपनी मानसिक गति को नियंत्रित करने के बजाय रोकने पर ऊर्जा का अनावश्यक क्षय कर देते हैं । मेरे अनुसार पयह वैज्ञानिक नहीं नहीं है । यहाँ तक कि काल्पनिकता को रोकने की प्रक्रिया में जो भी ध्यान किया जाता है उसमें सिर दर्द का होना स्वाभाविक हो जाता है । पहले से कहीं अधिक चिंताओं , आकांक्षाओं, भय और भ्रम के दलदल में मन को और धकेल दिया जाता है । किंतु प्रारंभ में ध्यान का वास्तविक उद्देश्य मन को पूरी तरह रोकना नहीं होना चाहिए ।—बल्कि इसको सुंदरतापूर्वक, सहजता से उसकी गति को नियंत्रित किया जाना चाहिए ।
मानसिक ऊर्जा का अनावश्यक व्यय: मन की अशांति का कारण
हमारे विचार केवल मानसिक क्रियाएँ नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा के सूक्ष्म रूप हैं। जब हम किसी विषय पर अत्यधिक सोचते हैं, तो यह एक प्रकार की मानसिक हलचल उत्पन्न करता है, जिसमें ऊर्जा का अपव्यय होता रहता है। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि व्यक्ति इसे सामान्य रूप से अनुभव नहीं कर पाता, किंतु इसका प्रभाव व दुष्प्रभाव उसके मस्तिष्क और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
उदाहरण के लिए—
कोई व्यक्ति आधे घंटे के लिए किसी एकांत स्थान में बैठा हो, किंतु उसके विचार लगातार दौड़ रहे हों—वह अतीत की किसी घटना को याद कर रहा हो, भविष्य की किसी चिंता में डूबा हो, या किसी काल्पनिक संवाद में उलझा हो—तो वह मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करेगा । वह इसलिए कि उसके सभी इन्द्रियों और मस्तिष्क के कई महत्वपूर्ण हिस्सों का उपयोग हुआ है भले ही उसने कोई शारीरिक परिश्रम न किया हो।
इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति घंटों तक पूर्णतः शांत चित्त के साथ बैठा रहे, तो भी उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होगी। वह न केवल तरोताजा महसूस करेगा, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सशक्त होगा। वह इसलिए कि शरीर के आंतरिक मशीनरी का उपयोग कम से कम हुआ है ।
इसी तरह ध्यान में अभ्यस्त मन किसी कार्य को करते समय भी अनावश्यक आंतरिक काल्पनिक संवादों बच जाते हैं । यही कारण है कि कई लोग शारीरिक रूप से अत्यधिक श्रम करने के बावजूद भी थकते नहीं हैं, जबकि कुछ लोग केवल सोचते-सोचते ही मानसिक और शारीरिक रूप से चूर हो जाते हैं ।
ध्यान और कल्पना का संतुलन
ध्यान का मूल उद्देश्य केवल विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि विचारों के प्रवाह को इतना नियंत्रित कर देना है कि वे व्यक्ति को आंतरिक शांति की ओर ले जाएँ, न कि मानसिक उलझन की ओर। जब कल्पना की गति को सही ढंग से साधा जाता है, तो यह व्यक्ति की ऊर्जा को भीतर केंद्रित करने में सहायता करती है।
ध्यान हमें यह सिखाता है कि—
• मानसिक गति को इस प्रकार संतुलित किया जाए कि ऊर्जा का न्यूनतम व्यय हो।
• कल्पना की शक्ति को एक दिशा में केंद्रित किया जाए, जिससे मन अनावश्यक कल्पनाओं से बच जाये । किसी भी विषय की गहराई में अनुभव करने का प्रयत्न करने ताकि मन अनावश्यक काल्पनिक वृत्तियों को न बना सके व उसे किशन ही न करे ।
• विचारों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि वे मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति प्रदान करें, न कि मानसिक थकान।
शुद्ध कल्पना और व्यर्थ कल्पना का अंतर
कल्पना की शक्ति नकारात्मक नहीं है, किंतु जब यह अनियंत्रित होती है, तो यह व्यक्ति के जीवन में अधिक भ्रम, तनाव और चिंता को जन्म देती है। मैंने देखा है कि अत्यधिक काल्पनिक शक्ति वाले मन का मस्तिष्क बहुत तीव्रता से थकता है और उसके थकान को मिटाने के लिए किसी न किसी ड्रग व नशा वाले पदार्थ को लेना पड़ता है । इसीलिए ध्यान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह है कि व्यक्ति अपनी शुद्ध कल्पना और व्यर्थ कल्पना के बीच अंतर करना सीखे।
• शुद्ध कल्पना – शुद्ध कल्पना का अर्थ सीमित और व्यावहारिक कल्पना से है जिसमें किसी कार्य के पहले व्यक्ति कार्य को संपन्न करने के लिए एक काल्पनिक खाका बनाता है और प्रारंभ में उसी के अनुरूप चलने का प्रयत्न करता है । यद्यपि व्यवहार में चलते हुए शीघ्र ही उस कल्पना की व्यर्थता समझ आने लगती अहि । क्योंकि कल्पना के अनुसार व्यवहार नहीं घटित होता है । काल्पनिक कष्ट तो व्यवहार में जाने के लिए प्रेरणादायक होती हैं । मन जब व्यवहार में घुसकर अनुभव करता है तब तब धीरे धीरे काल्पनिक वृत्तियों स्वतः ही कम होने लगती हैं । यह व्यवहार ही उसकी अनावश्यक काल्पनिक वृत्तियों को नियंत्रित करने लगता है ।
• व्यर्थ कल्पना – मैं उसे व्यर्थ कल्पना मानता हूँ जिसका व्यवहार से दूर दूर तक कोई सम्बंध ही न हो । और साथ साथ वह व्यवहार में जाने से आपको रोक दे ।
जैसे । जैसे कोई योग का अभ्यास कर रहा हो और वह उसी समय उसके द्वारा किसी कल्पना में व्यस्तता हो जाये तो उसका योग का अभ्यास रुक जाए तो समझ लो कि उसकी काल्पनिक क्षमता उसके व्यवहार पर बाहरी पड़ गई । इस प्रकार की कल्पनाएँ ही व्यवहार में जाने से रोकती हैं । व्यक्ति को भूतकाल की स्मृतियों, भविष्य की अनिश्चितताओं और निरर्थक चिंताओं में उलझा देती है।
जो व्यक्ति ध्यान की प्रक्रिया में गहराई से उतरता है, वह यह जानने लगता है कि उसके मन में कौन-से विचार अनावश्यक हैं और कौन-से विचार उपयोगी हैं। धीरे-धीरे, वह अपनी मानसिक ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ने में सक्षम हो जाता है, जो उसे आंतरिक संतुलन और मानसिक शांति की ओर ले जाए।
ध्यान की अवस्था: ऊर्जा की संचित अवस्था
ध्यान केवल विचारों को रोकने की विधि नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा को संचित करने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति कल्पना की गति को संतुलित कर लेता है, तो उसके भीतर एक गहरी स्थिरता उत्पन्न होती है। यह स्थिरता ही ध्यान की सही अवस्था है।
ध्यान हमें यह सिखाता है कि—
1. मन को शांत किया जाए, लेकिन जबरदस्ती दबाया न जाए।
2. कल्पना की शक्ति को नियंत्रित किया जाए, लेकिन इसे पूर्णतः रोका न जाए।
3. ऊर्जा को संयमित किया जाए, ताकि यह भीतर ही भीतर शक्ति का स्रोत बन सके।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy