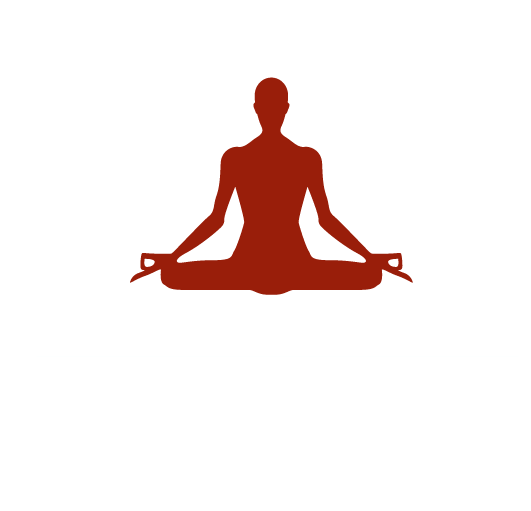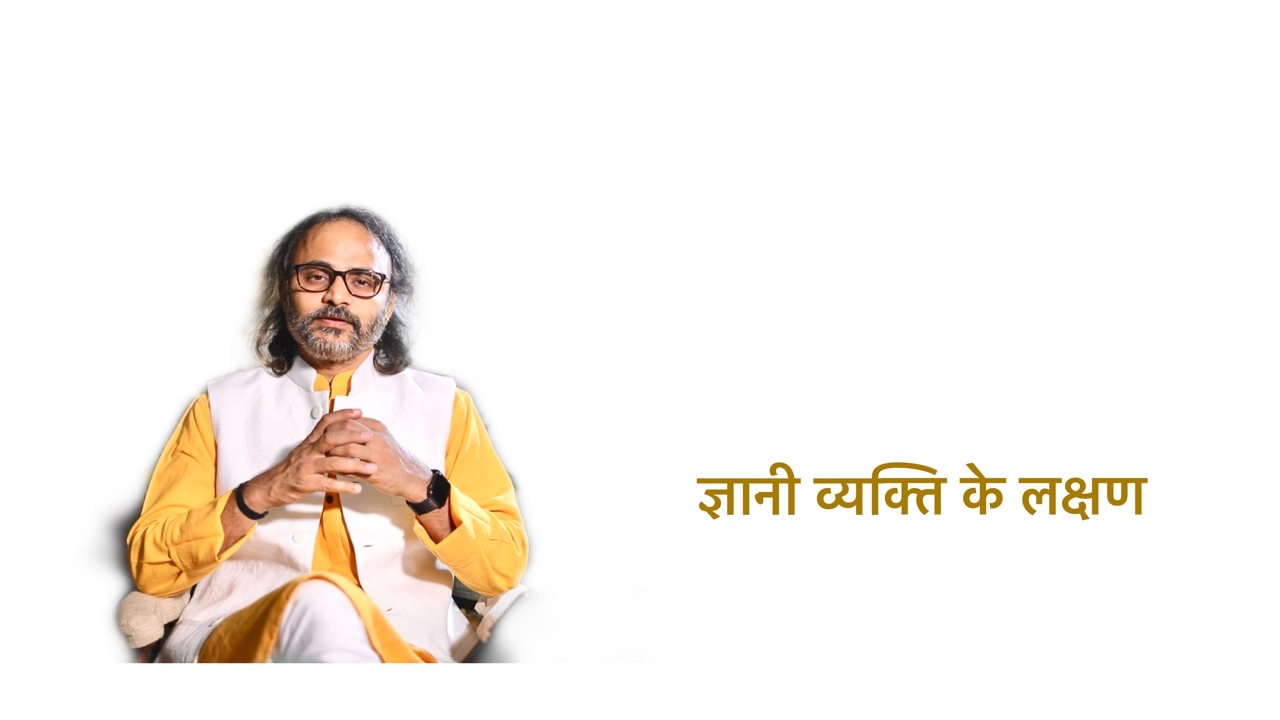
ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण
3 years ago By Yogi Anoopज्ञानवान व्यक्ति के लक्षण; मुमुक्षु के लक्षण
आध्यात्मिक दृष्टि में ज्ञान का मूल अर्थ है तत्व का ज्ञान । पुरुष अर्थात् जानने वाला और प्रकृति अर्थ जिसको जाना जाता है , ये दो ही तत्व है जिसका आध्यात्म साधकों के द्वारा जानने का प्रयास किया जाता है । यहाँ पर महर्षि पतंजलि के अनुसार उस व्यक्ति के लक्षणों की चर्चा किया जा रहा जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है ।
एक ज्ञानी का प्रमुख लक्षण है स्वयं (चेतन आत्म) तथा स्वयं के अतिरिक्त दृस्य (प्रकृति) मे आवस्यक भेद को जान लेना । यह तभी संभव है जब पुरुष और प्रकृति जैसे दोनो के गुण धर्मो को अच्छी तरह से जान लिया जाय । य्दयपि इसको जानने का साधन प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नही है । जब इसे जान लिया जाता है तो सात प्रकार की अनुभूति होती है ।
1- परिज्ञात प्रज्ञा : ‘जो जानने योग्य था उसे जान लिया’ न मै जड़ जगत में हूँ और न जड़ जगत मुझमे है अर्थात मुझको अनात्म मे आत्म का जो भ्रम था वह समाप्त हो गया और साथ साथ आत्म मे अनात्म का भ्रम भी समाप्त हो गया । इस प्रकार ज्ञात हो गया कि चेतन और जड दोनो की विपरीत दिशा है । जड़ जहॉं अनित्य तथा परिवर्तनशील है तो वहीं चेतन आत्म नित्य तथा अपरिवर्तनशील है ।इसके अतिरिक्त अन्य जानने योग्य कुछ भी तो नही है इस जगत मे और जगत के पार भी ।
2- हेय शून्य प्र्र्र्रज्ञा : ‘जो त्यागने योग्य था उसे त्याग दिया’ अब कुछ भी त्याग करना शेष नही रहा । पुरूष का प्रकृति से जो जन्म जन्मान्तर का मोह है उसे तभी त्यागना संभव है जब जो जानने योग्य है उसे जान लिया जाय । उसके बाद त्याग मे कोई कमी नही आ सकती है । यहॉं पर हेय का अर्थ त्यागने योग्य अर्थात बुद्धि के पास अब त्यागने योग्य कुछ शेष नही रहा ।
3- प्राप्यप्राप्तिप्रज्ञा : ‘जो प्राप्त करने योग्य था वह प्राप्त कर लिया’ जो जाने योग्य था उसे जान लिया उसके बाद त्यागने योग्य जो भी था उसे त्याग दिया और अब त्यागने के बाद जो मूल बचा जिसको त्यागा नही जा सकता था वह प्राप्त हो गया व उसे यह कह सकते कि ज्ञान हो हो गया । अर्थात जो प्राप्त करने योग्य था उसे प्राप्त कर लिया । किन्तु ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको त्यागा नही जा सकता है और जो प्राप्त करने योग्य है वह है स्वयं का स्वरूप । उसी मे स्थिति को प्राप्त करना कहतें हैं । समाधिपाद का तीसरा सूत्र इसके अर्थ को चरितार्थ करता है ।
‘तदा दृष्टु स्वरूपेअवस्थानम’
इसके अतिरिक्त प्राप्त करने के लिये अन्य कुछ भी नही हैं । इसी को असम्प्रज्ञात समाधि भी कहतें हैं ।
4- कार्यविमुक्ति अवस्था : ‘जो अन्तिम लक्ष्य था उसे पूरा कर लिया’ स्वरूप मे स्थिति होना ही पुरूष का मुख्य लक्ष्य है, उसके प्राप्त करने के बाद अब किसी कर्म की कोई आवश्यकता नही है । इस अवस्था मे कर्म का अवलेश मात्र भी नही है इसीलिये इसे क्रिया कर्म से विमुक्ति की अवस्था कहतें है ।
5- चित्तविमुक्तिप्रज्ञा : कुऐं की तब तक आवस्यकता होती जब तक उसमे जल होता है । पानी के सूख जाने पर कुँआ की कोई आवश्यकता नही रह जाती है । बिल्कुल उसी प्रकार वृत्तियों के आत्यान्तिक क्षय के बाद चित्त का कार्य समप्त हो जाता है । चित्त की कोई आवस्यकता नही रह जाती है । क्योंकि वृत्तियों का आना समाप्त हो गया । वृत्तियों का आश्रय उसके चित्त में ही है ।
6- गुणातीत प्रज्ञा : ‘समस्त गुणों के अतीत हो जाना और वो हो गया’ सत-रज-तम इन तीनों से परे हो जाना । यह कैसे संभव है ? जो पाना था उसे पा लिया फिर उसके बाद इन तीनों गुणों की कोई आवश्यकता नही रह जाती है । इनका कोई आश्रय न होने के कारण ये विलीन हो जातें हैं ।
7- स्वरूपमात्रज्योंतिः प्रज्ञा : गुणातीत होने से ज्योतिस्वरूप असंग केवली है । वह अपने आप का सदा अनभूति करता है ।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy