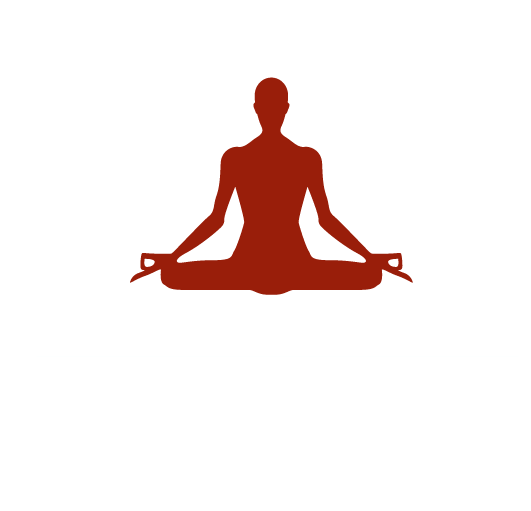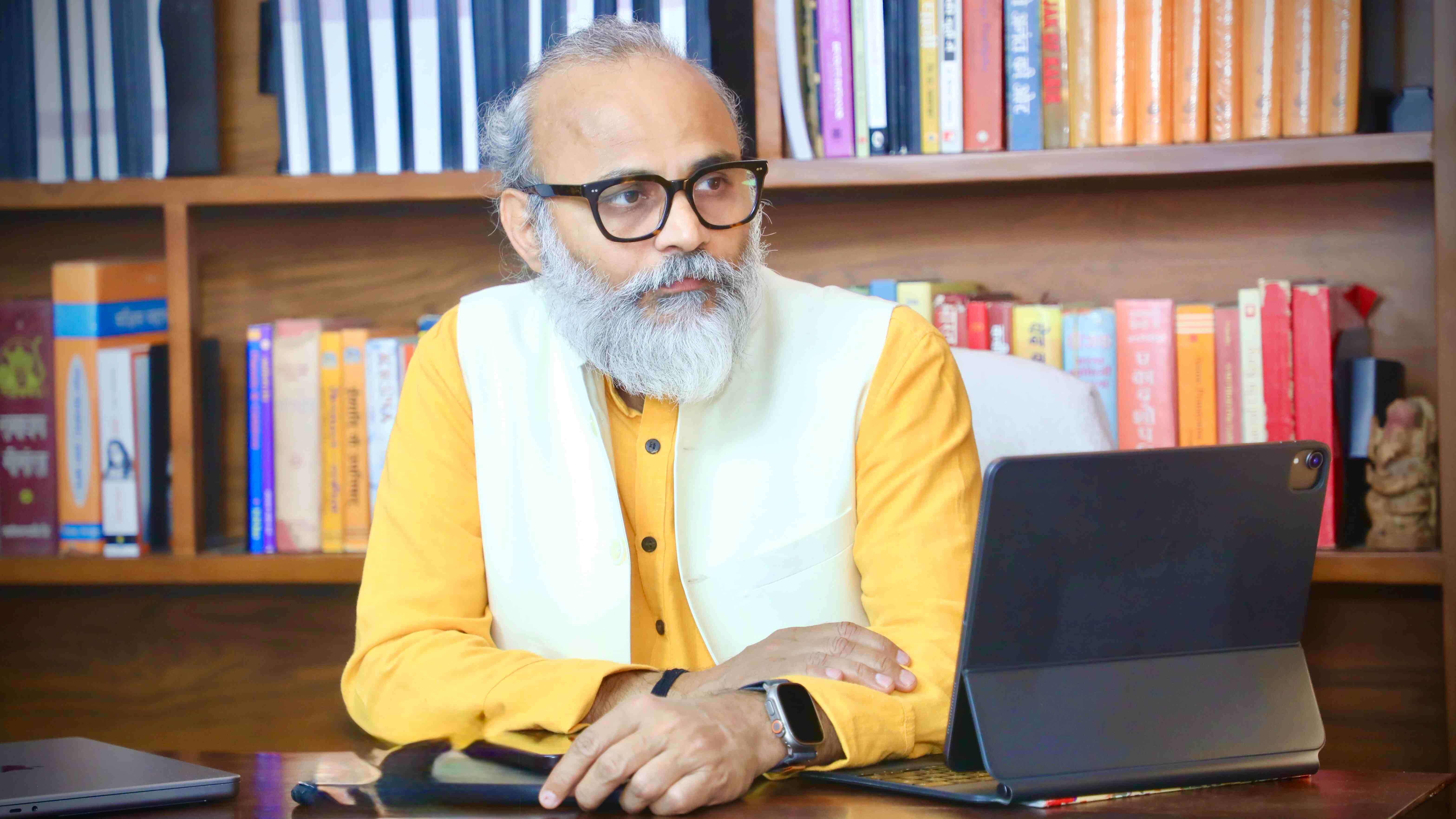
ज्ञान के तीन द्वार
10 months ago By Yogi Anoopज्ञान के तीन द्वार: देखने, सुनने और पढ़ने की शक्ति और आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव
अनुभवजन्य समझ:
हमारा मस्तिष्क दृश्य अनुभवों को सबसे जल्दी और प्रभावी ढंग से ग्रहण करता है। आँखों से देखने पर कोई भी चीज़ तत्काल स्मृति में दर्ज हो जाती है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही कारण है कि बच्चे किसी चीज़ को देखकर अधिक तेजी से सीखते हैं, जबकि वही चीज़ केवल शब्दों में समझाने पर धीमी गति से ग्रहण होती है।
दृश्य अनुभव से हमारा मस्तिष्क केवल सूचनाएँ ही नहीं लेता, बल्कि वह रंग, आकृति, गति और भावनाओं को भी एक साथ आत्मसात करता है। यही कारण है कि एक चित्र या चलचित्र हमें अधिक प्रभावशाली और दीर्घकालिक रूप से याद रह जाता है, जबकि मौखिक या लिखित जानकारी उतनी प्रभावी नहीं होती। यही वजह है कि शिक्षा में भी दृश्य-श्रव्य माध्यमों का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह मस्तिष्क में स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए आध्यात्म में सर्वप्रथम मार्ग भक्ति योग का दिया जाता है जिसमें चित्रों व चलचित्रों के माध्यम से मन मस्तिष्क के अंदर आध्यात्मिक उन्नति करवायी जाती है ।
श्रवण अनुभव:
सुनना देखने से थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क को ध्वनि के साथ-साथ संदर्भ को भी जोड़कर समझना पड़ता है। जब हम किसी व्यक्ति बिना देखे हुए सिर्फ बोलते हुए सुनते हैं, तो हमें उसके शब्दों के साथ-साथ उसके चित्र, उसकी भावनाएँ, लहजा, स्वर और गति को भी समझना पड़ता है।
रेडियो, पॉडकास्ट, प्रवचन या वार्तालाप से हमें विषय का सार अवश्य मिल जाता है, लेकिन दृश्य समर्थन न होने के कारण यह हमेशा उतना प्रभावी नहीं होता, जितना कि कोई दृश्य माध्यम। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें एक दृश्य दिखाकर समझाए कि कोई मशीन कैसे काम करती है, तो वह अधिक स्पष्ट और सहज लगेगा, जबकि केवल मौखिक विवरण से उसे समझने में अधिक ऊर्जा और कल्पनाशक्ति लगानी पड़ेगी।
श्रवण अनुभव के साथ एक समस्या यह भी होती है कि यदि सुनते समय ध्यान भटक जाए, तो पूरी समझ बाधित हो जाती है। पढ़ने या देखने में हम अपने अनुसार गति को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन श्रवण माध्यम में हमें वक्ता की गति पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए श्रवण माध्यम प्रभावी तो हो सकता है, लेकिन यह देखने के मुकाबले अपेक्षाकृत अधिक बौद्धिक ऊर्जा की माँग करता है। यद्यपि इसमें तार्किक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के बढ़ाने के अधिक संभावनाएं होती हैं ।
पाठ आधारित समझ:
पढ़ना सुनने से अधिक जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें केवल शब्दों के माध्यम से पूरी संरचना को मस्तिष्क में निर्मित करना पड़ता है। जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें वर्णित घटनाओं, पात्रों, विचारों और भावनाओं को पूरी तरह समझने के लिए हमें अपनी कल्पना शक्ति और बौद्धिक क्षमता को सक्रिय करना होता है।
यह एक प्रकार से मस्तिष्क के लिए व्यायाम की तरह है, क्योंकि यहाँ कोई दृश्य सहायता नहीं होती—सब कुछ केवल शब्दों और उनके अर्थों के माध्यम से ही समझना होता है। यही कारण है कि गहरी समझ के लिए पढ़ाई को सबसे श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है।
हालाँकि, पढ़ना केवल सूचना ग्रहण करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की सोचने, तर्क करने और विश्लेषण करने की क्षमता को भी विकसित करता है। जब हम पढ़ते हैं, तो हमारा मस्तिष्क केवल जानकारी ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह उसे आत्मसात करता है, विश्लेषण करता है और उससे नए निष्कर्ष निकालता है। इसलिए पढ़ने से व्यक्ति का मानसिक स्तर अधिक परिपक्व और विकसित होता है।
लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि पढ़ाई का प्रभाव व्यक्ति पर इस बात पर निर्भर करता है कि वह उसे कितनी गहराई से समझ रहा है। केवल सतही रूप से पढ़ने से उतना लाभ नहीं होता, जितना कि गहरे चिंतन के साथ पढ़ने से। इसी कारण, गहरे अध्ययन में रुचि रखने वाले लोग सामान्य पाठकों की तुलना में अधिक बौद्धिक और आत्मविश्लेषणात्मक होते हैं।
सहज मार्ग की प्रवृत्ति:
ध्यान दें, अभी तक मन अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाह्य दृश्यों तक पहुँचकर उन्हें समझने का प्रयत्न करता है और उस समझ के माध्यम से स्वयं के बौद्धिक स्तर की वृद्धि करता है।
यह माध्यम सरल है क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव ही मन को बाह्य वस्तुओं तक पहुँचाना है, चाहे वह आकृति, ध्वनि या शब्द के माध्यम से ही क्यों न हो। इन सभी माध्यमों में मन को बाह्य जगत में जाकर जुड़ना पड़ता है।
किन्तु आध्यात्मिक मार्ग की विद्या इसके बाद प्रारंभ होती है। जब यही दृष्टा स्वयं को समझने के लिए मन-बुद्धि को जानने का प्रयास करता है, तब वहाँ पर इस प्रकार के बाह्य साधनों का उपयोग लगभग नगण्य हो जाता है। यह सत्य है कि यह मार्ग अत्यंत कठिन है, क्योंकि मन-मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रवृत्ति कम ऊर्जा खर्च करके अधिक ग्रहण करने की होती है।
मन को लगता है कि बाह्य जगत को समझना सरल है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत से आसानी से जुड़ा जा सकता है। यही कारण है कि वह इस आसान मार्ग को चुनता है—इसीलिए उसे देखना सुनने से सरल लगता है और सुनना पढ़ने से।
किन्तु इस सहजता में एक बड़ा अंतर यह है कि जो चीज़ जितनी सरलता से ग्रहण होती है, वह उतनी ही जल्दी भुला भी दी जाती है। उसमें पूर्ण स्थायित्व नहीं दिखता। उसमें पूर्ण आत्मशांति और आत्मस्थिरता नहीं प्रतीत होती।
आत्मिक मार्ग: स्वयं को जानने की गूढ़ यात्रा
जब दृष्टा स्वयं को समझने के लिए इस देह में स्थित इंद्रियों, मन, स्वभाव, बुद्धि आदि को जानने का प्रयास करता है, तब वहाँ बाह्य जगत के किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती—न शब्दों की, न आकृतियों की, न रंगों की, और न ही किसी अन्य बाह्य संकेत की। आत्म-ग्रहण की इस यात्रा में व्यक्ति को केवल अपने स्वभाव को गहराई से समझना होता है, बिना किसी बाहरी समर्थन के।
यह कार्य अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि यह केवल बाहरी ज्ञान नहीं, बल्कि देह और मस्तिष्क के भीतर निरंतर घटित हो रही सूक्ष्म घटनाओं के परीक्षण और आत्मसाक्षात्कार का समय होता है। ध्यान दें कि सभी अनुभव और बोध केवल प्रत्यक्ष अनुभूति और आत्मपरीक्षण के आधार पर ही प्राप्त होते हैं।
यह देह अपने अनुभवों को न तो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करती है, न ही किसी स्पष्ट आकृति में प्रकट करती है। यह तो अपने स्वाभाविक प्रवाह में सतत चलायमान रहती है, और इस स्वाभाविकता को चेतन आत्मा, अर्थात् दृष्टा, को अपनी बौद्धिक एवं आत्मिक क्षमताओं के आधार पर समझना होता है।
आत्म-ग्रहण की इस प्रक्रिया में तर्क से परे गहन अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह यात्रा बाह्य से अंतर्मुखी होने की होती है—जहाँ विचार नहीं, केवल साक्षीभाव ही सत्य होता है।
अंततः:
मेरा कहना केवल इतना है कि उन चीजों को समझना बहुत कठिन होता है, जो आपके अत्यंत निकट होती हैं। जिनकी न तो कोई आकृति होती है, न शब्द, न श्रवण—उन्हें समझने की प्रक्रिया आसान नहीं है।
इसे समझने के लिए एक प्रखर आत्मज्ञानी गुरु की परम आवश्यकता होती है। वह बार-बार शिष्यों की तार्किक और बौद्धिक क्षमता को धारदार बनाता है और उन्हें स्वयं को समझने के लिए प्रेरित करता है।
अंततः, जीवन का अंतिम समाधान प्राप्त हो जाता है। इसके प्रमुख प्रमाणों में भारतीय उपनिषदों में गुरु-शिष्य की तार्किक, व्यावहारिक और ज्ञानात्मक चर्चाएँ विद्यमान हैं।
यहाँ तक कि ग्रीक दर्शन में भी गुरु और शिष्य के बीच चर्चाएँ देखने को मिलती हैं।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy