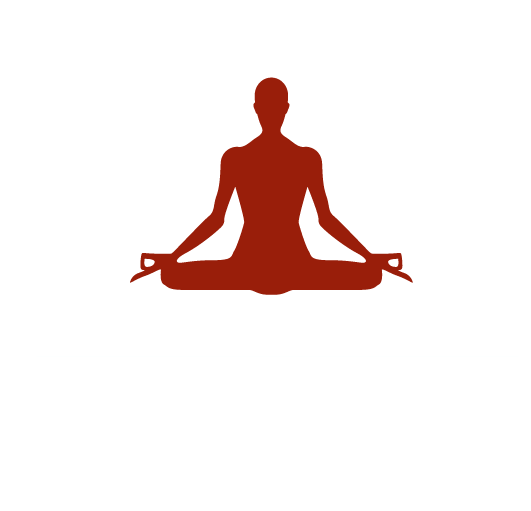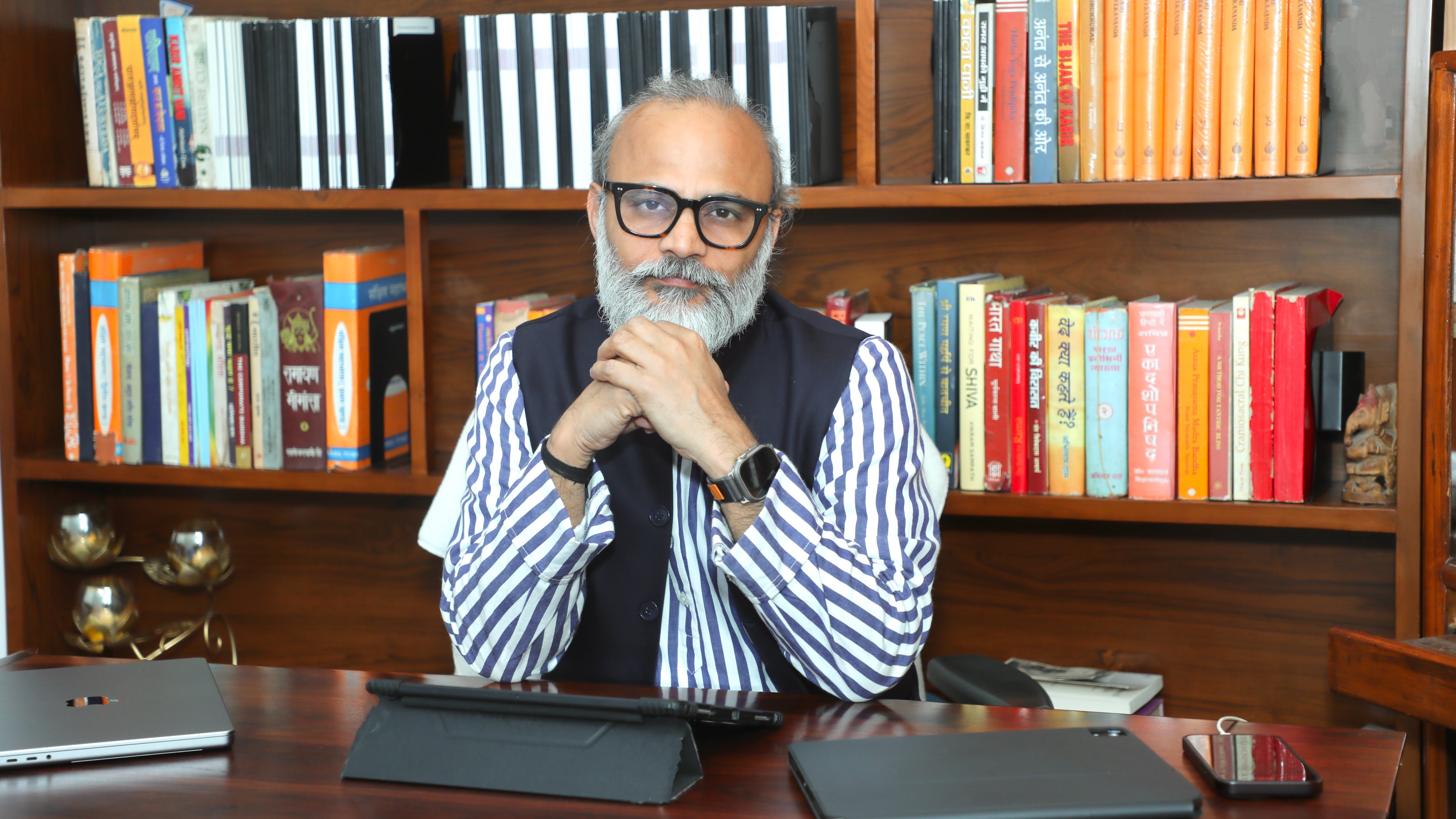
चित्त वृत्ति संयोग:मानसिक रोगों की उत्पत्ति
11 months ago By Yogi Anoopचित्त और वृत्तियों का संयोग:मानसिक रोगों की उत्पत्ति
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः – एक गहन विश्लेषण
महर्षि पतंजलि का यह सूत्र— “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः”—योग के सार को संक्षेप में व्यक्त करता है। इस सूत्र का वास्तविक अर्थ केवल सतही स्तर पर चित्त की वृत्तियों को रोकना नहीं है, बल्कि यह एक गहन मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। यदि हम इस परंपरा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और दार्शनिक आधार को समझें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह केवल एक व्यावहारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मानव मन के मूलभूत स्वभाव को समझने का प्रयास है।
मानव मन और उसकी अंतर्निहित समस्या
मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाह्य संसार में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर होता है। बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, यदि मन स्थिर है, तो वे अधिक प्रभाव नहीं डालतीं। किंतु यदि मन में हलचल है, तो बाह्य परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी अनुकूल हों, व्यक्ति अशांत ही रहेगा। महर्षि पतंजलि ने इस तथ्य को गहराई से समझा और इसे एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया।
संस्कृत में “चित्त” शब्द केवल मन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानसिक संरचना के लिए प्रयुक्त होता है। यह एक गतिशील शक्ति है, जो विभिन्न वृत्तियों (मानसिक धाराओं) के माध्यम से निरंतर क्रियाशील रहती है। यदि हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझें, तो चित्त को एक शांत सरोवर के समान माना जा सकता है, और वृत्तियाँ उसमें उत्पन्न होने वाली तरंगों के समान होती हैं। जब तक यह तरंगें हैं, तब तक जल में प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार, जब तक वृत्तियाँ सक्रिय रहती हैं, तब तक आत्मस्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकता।
चित्त और वृत्तियों का संबंध
महर्षि पतंजलि के अनुसार, चित्त और वृत्तियों का संबंध अत्यंत सूक्ष्म एवं जटिल है। वृत्तियाँ स्वयं उत्पन्न नहीं होतीं, बल्कि उनका आधार इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, स्मृतियाँ, इच्छाएँ और संस्कार होते हैं। जब बाहरी जगत की कोई वस्तु इंद्रियों के संपर्क में आती है, तो वह चित्त में एक प्रभाव छोड़ती है। यह प्रभाव किसी स्थूल पदार्थ की छाया के समान नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म मानसिक तरंग के रूप में रहता है। यही वृत्ति कहलाती है।
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या केवल बाहरी वस्तुएँ ही वृत्तियों को जन्म देती हैं? यदि ऐसा होता, तो जो वस्तु बाह्य रूप से उपस्थित नहीं होती, वह व्यक्ति के भीतर चिंता उत्पन्न नहीं कर सकती। किंतु हम जानते हैं कि स्मृतियाँ, कल्पनाएँ और पूर्व संस्कार भी उतनी ही प्रभावशाली होती हैं जितना कि प्रत्यक्ष अनुभव। इसी कारण वृत्तियाँ केवल इंद्रियों के संपर्क से नहीं, बल्कि स्मृति और कल्पना के द्वारा भी संचालित होती हैं।
वृत्ति और दुख का संबंध
अब यह स्पष्ट होता है कि वृत्तियाँ ही मानसिक अशांति और दुख का मूल कारण हैं। किंतु महर्षि पतंजलि केवल इस निष्कर्ष तक नहीं रुकते, वे इसका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। उनका तर्क यह है कि— यदि वृत्तियाँ चित्त में उत्पन्न होती हैं और वही दुख का कारण बनती हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि इन्हें समाप्त करके चित्त को शांत किया जाए?
यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि निरोध का अर्थ दमन नहीं है। यदि वृत्तियों को जबरदस्ती दबाने का प्रयास किया जाए, तो वे और अधिक शक्तिशाली होकर उभरती हैं। महर्षि पतंजलि का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है—वे वृत्तियों के स्रोत को समाप्त करने की बात करते हैं, न कि उन्हें बलपूर्वक रोकने की। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे यदि किसी नदी का जल प्रवाह नियंत्रित करना हो, तो उसके स्रोत पर नियंत्रण करना होगा, न कि केवल नीचे की ओर तटबंध बनाकर जल को रोकने का प्रयास किया जाए।
चित्त और वृत्तियों के वियोग की प्रक्रिया
यहाँ महर्षि पतंजलि का योगदर्शन सांख्य के साथ गहराई से जुड़ जाता है। सांख्य के अनुसार, पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही संसार की उत्पत्ति होती है। पतंजलि इस संयोग को मानसिक स्तर पर लागू करते हुए कहते हैं कि चित्त और वृत्ति का संयोग मानसिक संसार का आधार है। यदि यह संयोग समाप्त हो जाए, तो चित्त स्वतः शुद्ध और निर्मल हो जाता है।
यह प्रक्रिया साधारण नहीं है। यह केवल ध्यान लगाने की कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि एक संपूर्ण मानसिक पुनर्संरचना (Reconstruction of Mind) है। योगदर्शन में इसे “अभ्यास” और “वैराग्य”—इन दो साधनों के द्वारा संभव बताया गया है।
1. अभ्यास (Practice): अभ्यास का अर्थ केवल नियमित रूप से ध्यान लगाने से नहीं है, बल्कि मानसिक संरचना को धीरे-धीरे इस प्रकार विकसित करना है कि वृत्तियाँ स्वतः कमजोर होने लगें। यह उसी प्रकार है जैसे यदि किसी जलाशय को शांत करना हो, तो उसमें पत्थर फेंकने की प्रवृत्ति को धीरे-धीरे समाप्त करना होगा।
2. वैराग्य (Detachment): वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता है। यह वह अवस्था है, जिसमें व्यक्ति वृत्तियों से प्रभावित नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी कष्टदायक घटना को बार-बार स्मरण करता है, तो वह वृत्ति उसे कष्ट देती है। किंतु यदि वह घटना स्मरण में होते हुए भी व्यक्ति को प्रभावित न करे, तो वह वृत्ति निष्क्रिय हो जाती है।
महर्षि पतंजलि का यह सूत्र केवल योग साधना की तकनीकी व्याख्या नहीं है, बल्कि यह मानव मन के गहन वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। इसे केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित रखना इसकी व्यापकता को संकुचित करना होगा।
योग का वास्तविक अर्थ शरीर को स्वस्थ बनाना मात्र नहीं, बल्कि चित्त को इस प्रकार विकसित करना है कि वह वृत्तियों से प्रभावित न हो। जब यह अवस्था आ जाती है, तो मन स्वतः शांत हो जाता है और व्यक्ति वास्तविक मुक्ति का अनुभव करता है। यही पतंजलि का योग है—चित्त और वृत्ति के वियोग की प्रक्रिया।
राजा भोज ने इस सिद्धांत को इस प्रकार सराहा—
“पुंष्प्रकृत्योर्वियोगोअपि योग इत्युदितो यया।” (पुरुष और प्रकृति का वियोग ही योग है।)
अतः “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” केवल एक सूत्र नहीं, बल्कि एक संपूर्ण मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक प्रक्रिया का सार है, जो मनुष्य को मानसिक बंधनों से मुक्त करने की दिशा में अग्रसर करती है।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy