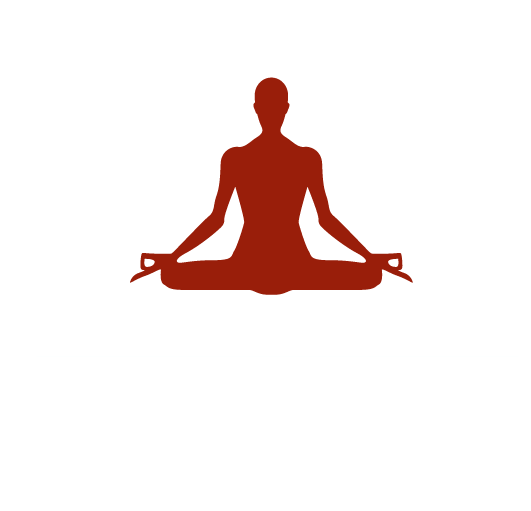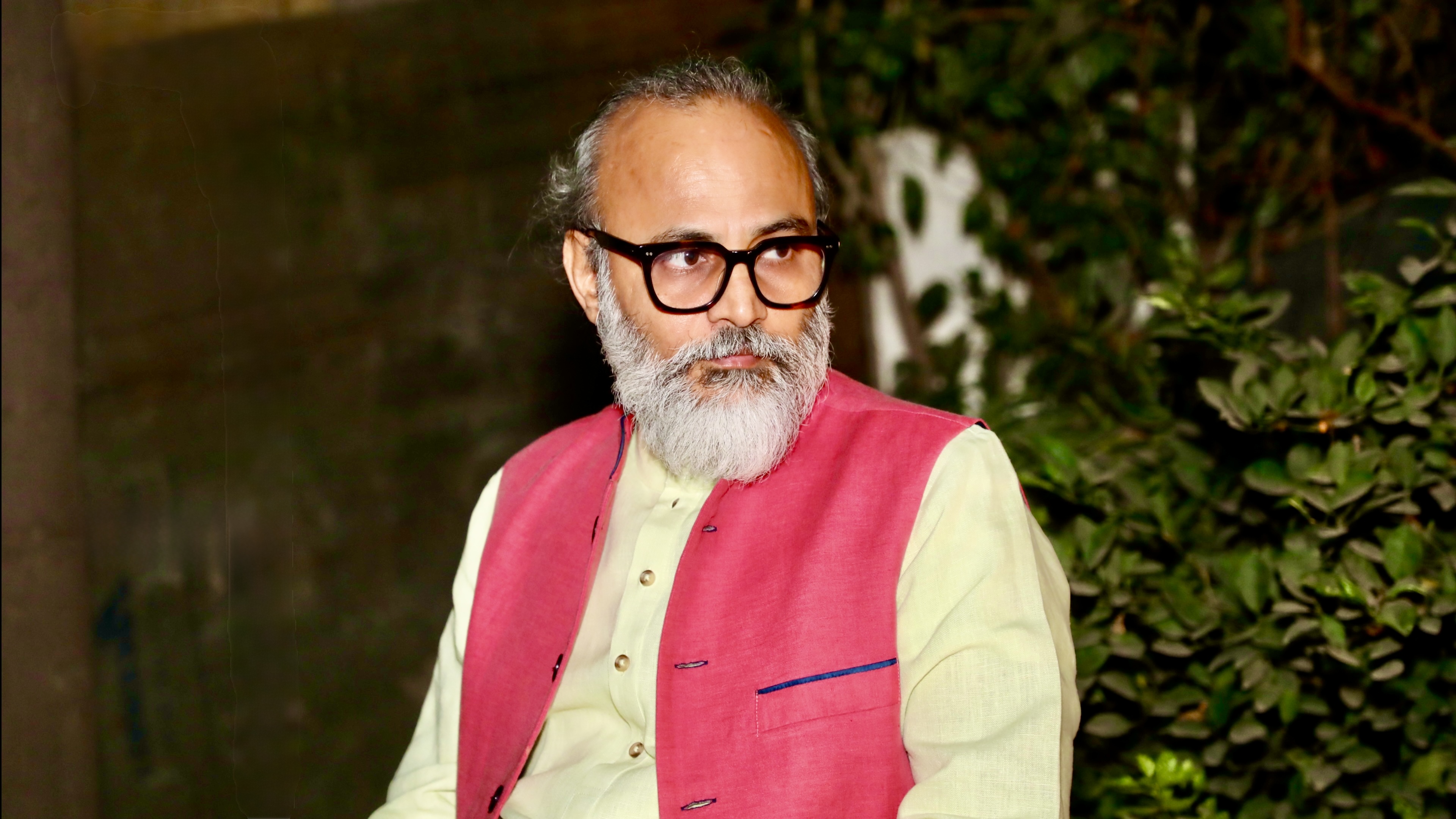
बोलने की यथार्थ गति और जीवन दर्शन
1 year ago By Yogi Anoopबोलने की यथार्थ गति और जीवन दर्शन
शिष्य: गुरुजी, मैंने सुना है कि आपकी बोलने की गति 56 से 60 शब्द प्रति मिनट है। क्या यह गति थोड़ी धीमी नहीं है?
योगी अनुप: यह धीमी प्रतीत हो सकती है, लेकिन इसे धीमा कहना सही नहीं होगा। देखो, मेरे विषय गहन, अनुभवात्मक और चिंतनशील होते हैं—दर्शन, योग, ध्यान, और आध्यात्म। इन विषयों पर जब हम बात करते हैं, तो धीमी गति श्रोताओं को चिंतन और शब्दों के गहरे अर्थ को समझने एवं आत्मसात करने का समय देती है। यही तो इन विषयों की खूबसूरती है। बातों में इतनी गहराई और व्यावहारिकता होनी चाहिए कि श्रोता सुनकर चिंतन करने पर मजबूर हो जाए। जैसे ही उनके भीतर प्रश्न उत्पन्न हों, गुरु को उनका उत्तर देना चाहिए। यदि वार्तालाप में गति तेज होगी, तो श्रोता में समझ विकसित हो ही नहीं सकती। इसीलिए बोलने की गति को धीमा रखना पड़ता है।
शिष्य: लेकिन गुरुजी, जब श्रोता तेज गति से बोले गए विचारों को सुनते हैं, तो क्या वह अधिक ऊर्जा और प्रेरणा का अनुभव नहीं करते?
योगी अनुप: यह एक सतही अनुभव हो सकता है। तेज गति वाले संवाद में ऊर्जा और जोश दिख सकता है, लेकिन उसमें गहराई नहीं होती। यह इसलिए क्योंकि बोलने वाले का ध्यान सिर्फ श्रोताओं को खुश करने पर होता है। मोटिवेटर्स अपनी बातों की तीव्रता और प्रभावशीलता से श्रोताओं के दिमाग को बाँधे रखना चाहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया से न तो श्रोता और न ही वक्ता का मानसिक कल्याण हो सकता है।
तेज गति से बोले गए शब्दों को आत्मसात करना मुश्किल होता है। बोलने वाले के मस्तिष्क पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि तेज संवाद अनुभव से प्रेरित नहीं होते। ऐसे शब्द कहीं और से लिए गए होते हैं और केवल दोहराए जाते हैं।
यही कारण है कि इतनी तीव्र गति से आने वाले विचार श्रोताओं को सोचने का समय नहीं देते। और अगर विचार उनके अंतर्मन तक पहुँच ही नहीं पाते, तो वे उन्हें आत्मसात कैसे करेंगे?
शिष्य: क्या इसका मतलब यही है कि तेज गति से बोलने का अभ्यास करना अनुचित है?
योगी अनुप: इसका अर्थ यह नहीं है कि तेज गति हमेशा अनुचित है। कभी-कभी परिस्थितियों के अनुसार तेज गति आवश्यक हो सकती है। लेकिन जब बात गहन और अनुभवात्मक विषयों की हो—जैसे दर्शन, ध्यान, योग, या आत्मज्ञान—तो धीमी गति अधिक प्रभावशाली होती है। इन विषयों में गुरु अपने अनुभवों को संवाद के माध्यम से शिष्यों को समझा रहा होता है। यह प्रक्रिया गणितीय अभ्यास की तरह है—जहाँ गहराई से समझने में समय लगता है।
कहानी सुनाने में गति तेज हो सकती है, लेकिन उसमें भी यदि भावनाओं को श्रोताओं के अंतरतम तक पहुँचाना है, तो गति धीमी करनी होगी। आध्यात्मिक विषयों में संवाद के दौरान शिष्य के मन में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इसलिए गुरु को इतनी धीमी गति से बोलना चाहिए कि शिष्य अपने प्रश्नों का उत्तर उसी क्षण खोज सके या उसे गुरु से पूछ सके।
शिष्य: तेज गति से बोलने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स की शैली के बारे में आपका क्या विचार है? वे तो अक्सर 160-180 शब्द प्रति मिनट तक बोलते हैं।
योगी अनुप: यह एक विकट समस्या है। इस शैली से वक्ता की अपनी स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। उसकी इंद्रियाँ इतनी तेज गति की आदत डाल लेती हैं कि भविष्य में वह उन्हीं समस्याओं से घिर जाता है जिन पर वह प्रवचन दे रहा होता है। तेज गति से संवाद करने से मानसिक और शारीरिक समस्याएँ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं।
ध्यान और चिंतन के लिए एक स्थिर और धीमी गति बेहतर होती है। यह तभी संभव है जब शब्द अनुभव से प्रेरित हों। अनुभव से प्रेरित शब्द स्वतः ही धीमी गति से निकलते हैं।
शिष्य: तो गुरुजी, क्या यह कहना सही होगा कि धीमी गति संवाद के गहरे प्रभाव के लिए आदर्श है?
योगी अनुप: बिल्कुल सही। धीमी और स्थिर गति श्रोताओं को न केवल सोचने का समय देती है, बल्कि उनके मन और आत्मा को छूती है। यह आत्मज्ञान और व्यवहारिक बदलाव के लिए आवश्यक है। याद रखना, संवाद का असली उद्देश्य यह है कि वह श्रोता के अंतरतम तक पहुँचे और वहाँ स्थायी प्रभाव छोड़े। यही संवाद श्रोता को अपने जीवन में व्यावहारिक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy