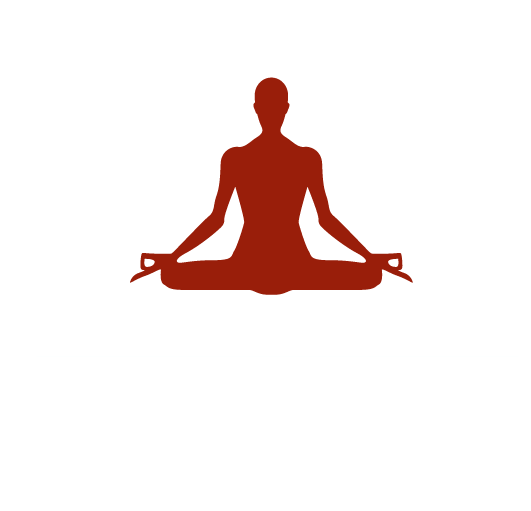भ्रम-स्वयं के प्रति अज्ञानता ही रोग है
4 years ago By Yogi Anoopस्वयं के प्रति अज्ञानता ही सबसे बड़ा रोग है
वस्तु के मूल स्वभाव को न पहचानना भ्रम व विर्पयय कहलाता है । जैसे रस्सी को सर्प समझना अथवा सर्प को रस्सी समझना भ्रम है। भ्रम की इस दशा को विर्पयय कहते हैं। भ्रम की यह स्थित दो कारणो से पैदा हो सकती है । एक पारिस्थितिक और दूसरा अविद्धया वश अधंरे मे रस्सी को सर्प समझ लेना‛ मे परिस्थति अधिक दोषी है क्योकि परिस्थति के कारण पुरूष को इस प्रकार का भ्रम हो रहा है। इसी परिस्थति के बदलने पर उसका भ्रम समाप्त भी होता है । जैसे प्रकाश होने पर रस्सी को वह रस्सी ही समझता है सर्प नही । इसलिये इस दोष का मूल कारण परिस्थति ही है पुरुष नही । इसमे पुरूष को दोषी नही समझा जा सकता है । इस तरह का भ्रम मनुष्य को अल्पकाल के लिये दुख देता है । यह दुख तभी तक होता है जब तक परिस्थति अनुकूल नहीं होती है । किन्तु जब परिस्थति अनुकूल हो जाती है तब सत्य प्रकट हो जाता है । इस प्रकार का भ्रम मनुष्य को ज्यादा देर तक दुख नही दे सकता है ।
किन्तु दूसरा कारण जिसका उत्तरदायित्व सिर्फ पुरूष को ही है अन्य किसी को नही वह है अविद्वया व अज्ञानता । अविद्वया का मतलब अज्ञानता अर्थात जो भ्रम स्वयं की अज्ञानता के कारण पैदा हो स्वयं की बददिमाकी के कारण पैदा हो जिसके दोषी हम स्वयं हो अन्य कोई न हो वह कारण अविद्वया का कारण है । जैसै : जड़ मे चेतन सत्ता की कल्पना करना तथा स्वयं (चेतन) को जड़ स्वीकार करना । दीवाल पर टंगे चित्र को चेतन मानकर अपने दुखों को हरने का आग्रह करना । जब कि आग्रह करने वाला ज्यादा शक्तिशालाी है। यहॉ पर परिस्थति अर्थात् दीवाल में टंगा चित्र दोषी नहीं है , दीवाल को दोषी नही बल्कि स्वयं की अज्ञानता को ही दोषी कहा जा सकता है ।
मन मस्तिष्क अभी इतना विकसित नहीं कि वह दीवाल पर टंगी हुयी चित्र से पैदा होने वाली संवेदनाओं को अलग कर सके । वह उन्ही चित्रों में से संवेदनाओं को पैदा करके स्वयं को आनंदित करता है , खुश करता है । वह अपने ही बनाई हुई कल्पनाओं में ही उलझने लगता है और सत्य ये है कि वह स्वयं से ही दूर होता जाता है ।
वह इस संसार में जितना उलझता जाता है उतना ही भविष्य में दुखी और रोगी होता जाता है । वह संसार में तो उलझता जाता है और उतना ही स्वयं को भूलता जाता है , और दुःख और डर के निवारण के लिए पूजा पद्यतियो व कर्मकांडों को स्वयं पर थोपता जाता है ।
प्रमुख दोष यह है कि दृष्टा जो दर्पण में स्वयं को देख सकता था वह दर्पण को ही देखने में फँस गया । वह जो संसार में रहकर स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर सकता था, वह अब इस संसार में स्वयं को ही विस्मृत कर गया है ।
जिसमे स्वीकार करने की शक्ति थी जो यह यह सिद्वध कर सकता था कि वह चेतन है स्वयं को अब स्वयं को जड़ मानते धूमता है और दृष्य चित्र को जिममे कोई चेतन नही है को चेतन मानता है ।
ध्यान दें दृष्य इसलिये चेतन नही हो सकता क्योकि किसी भी चित्र व दृष्य मे स्वयं को मानने की शक्ति नही होती है । उस दृष्य को मानने या न मानने का काम दृष्टा (पुरुष) का ही होता है । किसी भी दृश्य का मूल स्वभाव जड़ है किन्तु पुरूष उसमे चेतन सत्ता की कल्पना करता है । दृष्टा कुछ भी मान सकता है यदि उसके मानने का अधार ज्ञान है और वस्तु के निज स्वरूप को पहचान कर उसको उसी रूप मे देखता है तब अक्लिष्ठ होती है और मोक्ष मे सहयोगी होती है । समाधि शीध्र सिद्ध हो जाती है । किन्तु यदि उसके मानने का आधार अविद्वया व अज्ञानता से प्रेरित है और वस्तु के उस मूल स्वरूप पर पुरूष स्वयं द्ववारा कल्पित अन्य स्वरूप आरोपित करता है तब वह बन्धन कारक होती है । यह जन्म जन्म तक मनुष्य को भटकाती है ।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy