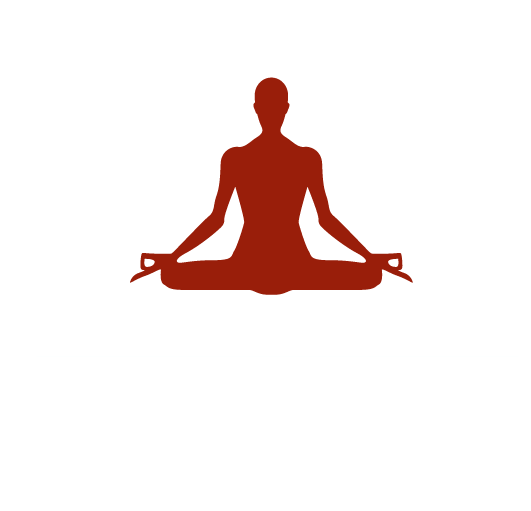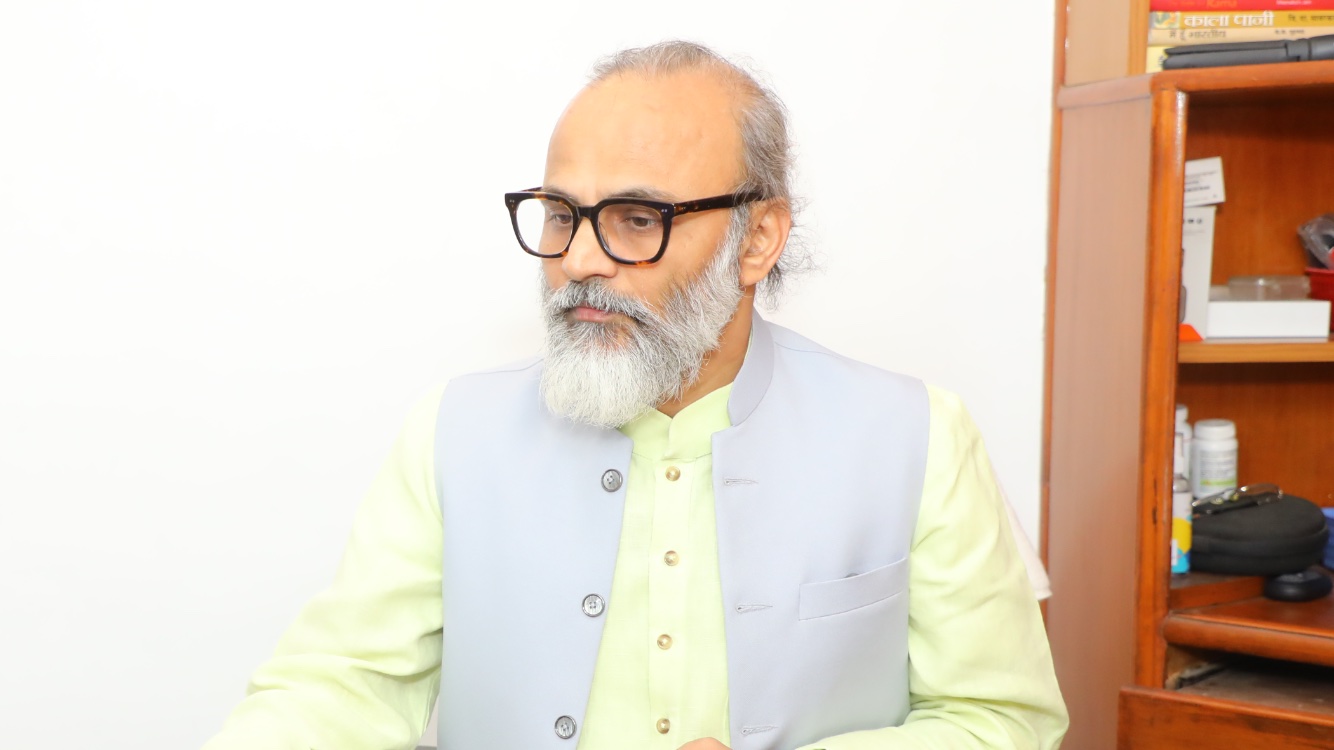
भोजन और स्वाद: एक दार्शनिक विवेचन
11 months ago By Yogi Anoopभोजन और स्वाद: एक दार्शनिक और वैज्ञानिक विवेचन
अनुशासन और विवेक के बिना आध्यात्मिकता अधूरी है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी विचारधारा को प्रमाणित करने के लिए किसी महान आत्मा या धार्मिक व्यक्तित्व के कथनों का सहारा ले लिया जाता हैं, भले ही उन कथनों का कोई प्रामाणिक स्रोत न हो। ऐसा ही एक कथन है—“भोजन कभी भी स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए।” यह विचार सुनने में सरल और आध्यात्मिक प्रतीत होता है, किंतु यदि इसे तार्किक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह अधूरा सिद्धांत है।
स्वाद और भोजन का संबंध: एक प्राकृतिक सत्य
भोजन केवल पेट भरने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण जैविक और मानसिक प्रक्रिया है। यह सत्य है कि भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं किया जाता, किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि स्वाद के बिना भोजन अधूरा है। जिह्वा (जीभ) को मात्र एक इंद्रिय समझना गलत होगा, क्योंकि इसका कार्य मात्र स्वाद लेना ही नहीं, बल्कि शरीर को भोजन के प्रति मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना भी है।
वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो स्वाद का कार्य मात्र इंद्रिय-सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पाचन तंत्र का एक अनिवार्य चरण है। जब भोजन जीभ पर आता है, तब स्वाद ग्रंथियाँ सक्रिय होती हैं और मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं कि भोजन ग्रहण किया जा रहा है। यह संकेत लार ग्रंथियों (salivary glands) को सक्रिय करता है, जिससे लार का स्राव बढ़ता है और भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।
यदि भोजन बिना स्वाद लिए निगल लिया जाए, तो मस्तिष्क पाचन के लिए आवश्यक संकेतों के माध्यम से एंजाइम्स के स्राव को उतनी तत्परता से नहीं भेजेगा, जिससे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और यह पेट की समस्याओं का कारण बन सकता है। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति को नींद में या अनजाने में भोजन कराया जाए, तो उसका पाचन तंत्र सही ढंग से कार्य नहीं करता है । यह एक स्पष्ट वैज्ञानिक सत्य है। यदि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मन द्वारा किसी भी विषय पर एक सीमा तक अनुभव की अवधि बनी रहे तो आत्म संतुष्टि की अनुभूति होगी अन्यथा वह भोजन से असंतुष्ट ही रहेगा । जिह्वा पर भोजन के पड़ने के बाद उसके स्वाद के संकेतों का मस्तिष्क में अधिक समय तक ठहरना होता है तब मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र में ढीलापन , शिथिलता व मन में संतुष्टि का स्तर बहुत चरम पर बढ़ जाता है । किंतु वहीं पर इसके विपरीत यदि भोजन का जिह्वा पर कम समय के लिए रखा गया हो और मस्तिष्क में बहुत कम समय के लिए उसके संकेतों का अनुभव किया गया हो तब उस अवस्था में मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र में ढीलापन नहीं हो सकता है और मन के संतुष्टि का स्तर कम होता जाएगा ।
स्वाद इंद्रिय का अस्वीकरण: प्रकृति के नियमों का उल्लंघन
यह मान लेना कि स्वाद लेना मात्र भौतिक सुख है और इसे छोड़ देना चाहिए, एक अव्यवहारिक विचारधारा है। जिह्वा में स्वाद ग्रंथियों का होना यह सिद्ध करता है कि उसका मन मस्तिष्क से भोजन को जोड़ा जाना एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है । यह प्रकृति प्रदत्त है । जीभ में स्वाद ग्रहण करने की शक्ति का होना यह प्रमाणित करता है कि यह प्रक्रिया शरीर के लिए आवश्यक है। यद्यपि धार्मिक दृष्ट से भोजन में स्वाद लेना ब्रह्मचर्य सिद्धि के लिए उचित उचित नहीं है । किंतु यह उस स्वाद के बारे में है जो अप्राकृतिक होता है, अत्यंत मसालेदार होता है ।
केवल इतना ही नहीं, जीभ तापमान संवेदना (temperature sensation) में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि कोई पदार्थ अत्यधिक गर्म या ठंडा हो, तो जीभ उसे तुरंत पहचानकर हमें सतर्क कर देती है। इसका अर्थ यह है कि जीभ केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि भोजन के संपूर्ण गुणों का आकलन करने का कार्य करती है। यह प्रक्रिया न केवल जीव विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दर्शनशास्त्र की दृष्टि से भी यही दर्शाती है कि शरीर और मन का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
स्वाद और आत्मसंयम: एक मध्य मार्ग
अब प्रश्न उठता है कि क्या स्वाद के प्रति आसक्ति गलत है? हाँ, यदि स्वाद मात्र इंद्रिय-सुख के लिए लिया जा रहा है और व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो रहा है, तो यह अनुचित है। लेकिन यदि स्वाद का सही उपयोग किया जाए—स्वस्थ और संतुलित आहार को आनंदपूर्वक ग्रहण किया जाए—तो इसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ पर स्वाद को लेने के लिए स्वाद के अनुभव का समय यदि बढ़ा दिया जाता है तब स्वाद के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है । मेरे अनुसार स्वाद के प्रति आसक्ति का अर्थ स्वाद के प्रति मन में हमेशा संवेदना का बने रहना अर्थात् वह स्वाद से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है । यह समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि स्वाद लेने की समयावधि बहुत कम होती है । और उस स्वाद का मस्तिष्क में गहन संवेदना की अनुभूति नहीं हो पाती है ।
यहाँ गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश प्रासंगिक हो जाता है—“युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु” अर्थात जो व्यक्ति आहार-विहार में संतुलन रखता है, वही सच्चे अर्थों में योगी है। संतुलित आहार का अर्थ केवल पौष्टिकता ही नहीं, बल्कि स्वाद और स्वास्थ्य का सामंजस्य भी है।
भोजन और स्वाद के विषय में किसी भी एकतरफा विचारधारा को अपनाना उचित नहीं है। न तो स्वाद को पूरी तरह नकारा जाना चाहिए, न ही उसे मात्र भोग-विलास का साधन बनाया जाना चाहिए। स्वाद, पाचन तंत्र का एक अभिन्न अंग है और इसका महत्व वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है।
यदि किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि वह स्वाद के बिना भोजन करे, तो यह प्रकृति के विरुद्ध होगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति केवल स्वाद के पीछे भागे और स्वास्थ्य की उपेक्षा करे, तो यह भी आत्मघातक सिद्ध होगा। इसीलिए, मध्य मार्ग ही श्रेष्ठ है—स्वाद के प्रति जागरूक रहें, किंतु उसके दास न बनें।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy