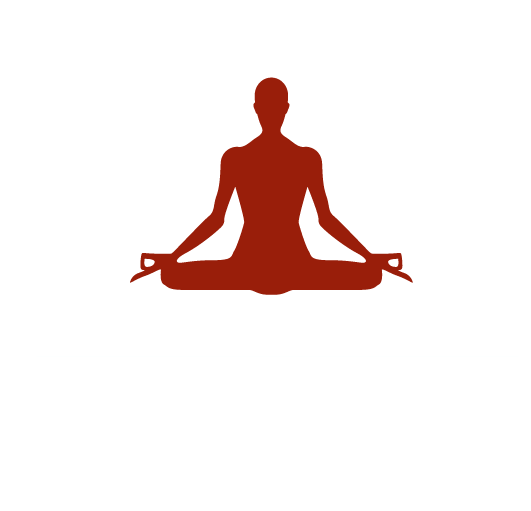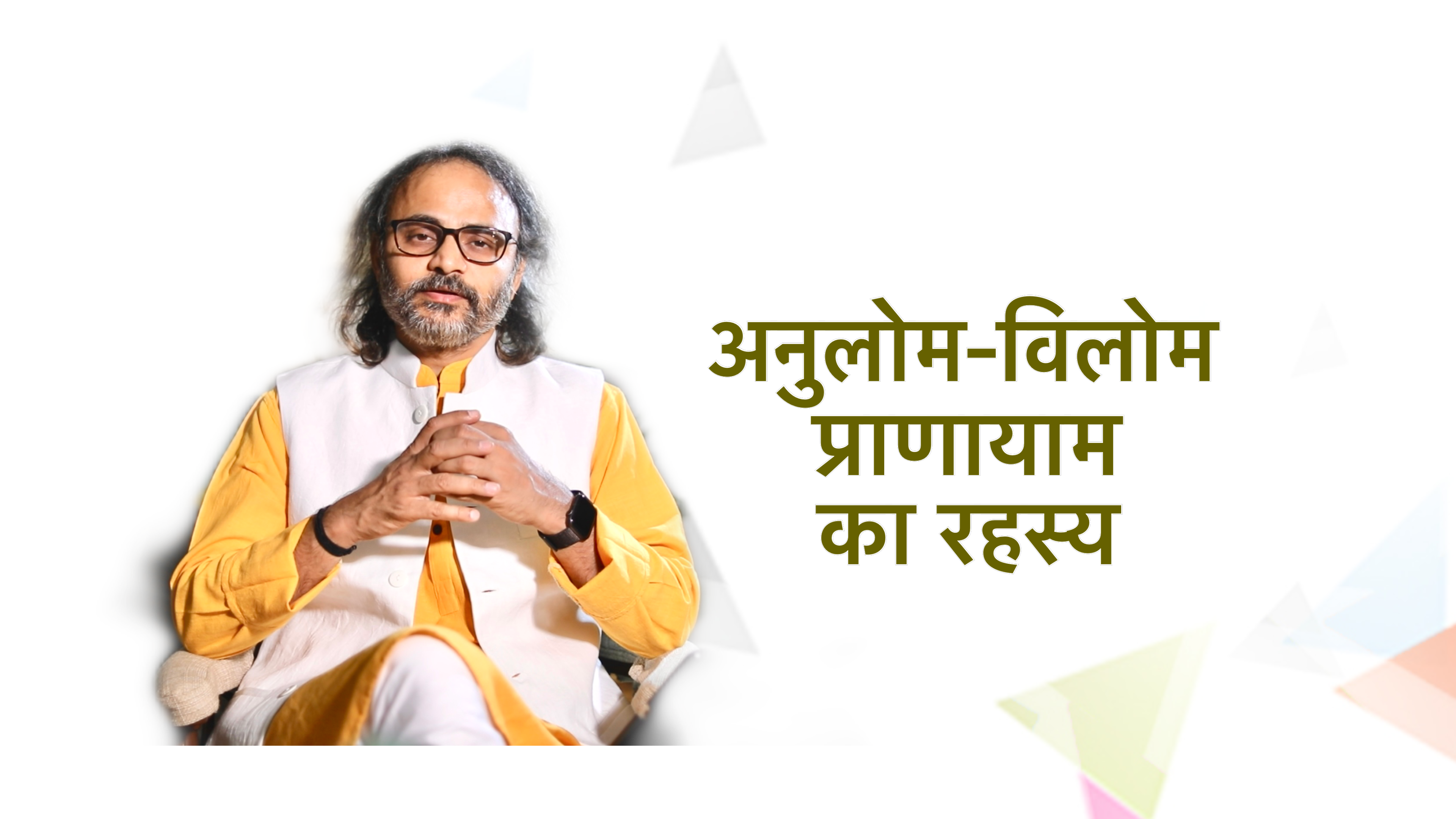
अनुलोम-विलोम प्राणायाम का रहस्य
4 years ago By Yogi Anoopसामान्यतः प्राणायाम में स्वाँस पर ज़ोर देने की बात की जाती है , ज़ोर देने का अर्थ यहाँ पर सिर्फ़ इतना ही है कि स्वाँस की गति में वैज्ञानिक विधि से छेड़ छाड़ किया जाना जिससे फेफड़े ही नहीं बल्कि नासिका से लेकर पर फेफड़े तक की दूरी पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सके ।
जहां तक अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात है इसमें प्राण पर नियमन तो सिखाया ही जाता है किंतु उससे कहीं अधिक नासिका के अंदर के अग्र भाग से लेकर गले तक के सभी सूक्ष्म स्थानों को अनुभव करना सिखाया जाता है । इन सभी सूक्ष्म स्थानों पर स्वाँस को जिसमें humid है अर्थात् पानी है, को नासिका से लेकर गले तक के अंदर के हिस्से में स्पर्श करवाया जाता है । इस स्पर्श से नासिका के अंदर सूक्ष्म कोशिकाओं में तरंगें पैदा होती है जो सीधा मस्तिष्क और आँखों को प्रभावित करती है ।
यहाँ तक कि इस प्राणायाम के अभ्यास से आँखों से आँसू भी निकलने लगते हैं ।
मेर अनुभव में स्पर्श के माध्यम से नाड़ियों को सर्वाधिक प्रभावित किया जाता है, कुछ वैसे ही जैसे आपके बाहरी त्वचा को कोई स्पर्श करता है तब त्वचा में कम्पन होकर रोएँ खड़े हो जाते हैं ।
प्राणायाम का यह विज्ञान स्पर्श से त्वचा में कम्पन पैदा करवाने की कोशिश करता है जैसे हीलिंग विज्ञान का मूल आधार स्पर्श ही तो है । किंतु उस हीलिंग विज्ञान में रोगी के ऊपर कोई अन्य स्पर्श चिकित्सा (हीलिंग) करता है और उसके माँ मस्तिष्क को प्रभावित करता है , शांत स्थिर करता है किंतु प्राणायाम की इस विधि में व्यक्ति स्वयं को स्वांसों के माध्यम से स्पर्श चिकित्सा देता है जो मस्तिष्क को सर्वाधिक प्रभावित करता है । मस्तिश में सूक्ष्म तरंगों को विकसित करके दाएँ और बाएँ मस्तिष्क में संतुलन स्थापित करता है साथ वात पित्त और कफ़ को संतुलित करता है ।
विधि
किसी एक स्थान पर सुखपूर्वक बैठकर अपनी दाहिनी नासिका को उँगलियों से बंद करके बायीं नासिका से धीरे धीरे साँसों को अंदर लेते हुए नाक के अंदर स्पर्श का अनुभव करना है । यदि नाक में अधिक सूखापन है तब उँगली में पानी लेकर नाक के अंदर लगा लें जिससे रूखापन कम हो जाय , और स्वाँस को अंदर लेते समय अंदर के पूरे हिस्से में स्पर्श का अनुभव करें । जितना स्पर्श का सूक्ष्म अनुभव होता जाएगा उतना ही साँस धीरे धीरे और शांत तरीक़े से अंदर जाएगी और साथ साथ चेहरे और इंद्रियों में ढीलापन आता जाएगा ।ध्यान दें इस प्राणायाम में अनुभव पर ज़ोर देना है न कि साँस को अंदर लेते समय गिनती पर ।
अब जब साँस अंदर चली जाय तब उसे 2 से 3 सेकंड के लिए आराम से रोकें, इस रोकने की प्रक्रिया को ही कुम्भक कहते हैं और उसके बाद दूसरी अर्थात् दाहिनी नाक से साँस को बिना कोई प्रयत्न के बाहर निकाल कर साँस को बाहर 2 से 3 सेकंड के लिए रोक लें । पुनः दाहिनी नाक से स्वस्थ को लेकर बायीं नासिका से निकल दें । यह एक चक्र कहलाता है ।
इस प्राणायाम को कम से 11 मिनट तो अवश्य किया जाना चाहिए ।
लाभ
ऐसा किताबों में वर्णित है कि इस प्राणायाम के 3 महीने के अभ्यास मात्र से बहत्तर हज़ार नाड़ियां स्वस्थ हो जाती हैं । यह पर 72 हज़ार नाड़ियों का अर्थ है कि सभी नसें नाड़ियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है , जो भी प्राणायाम मस्तिष्क को प्रभावित करता वो नसों और नाड़ियों को पस्वास्थ्य प्रदान करेगा ही । इससे इंद्रियों में स्थिरत और एकाग्रता भी बढ़ती है । मस्तिष्क का दोनों गोलार्द्ध में समन्वय स्थापित होता है, मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का अर्थ है कि दाहिने और बाएँ मस्तिष्क के हिस्से में अच्छी तरह से समन्वय ।
हानि
यदि ग़लत विधि से प्राणायाम किया जाय तो शरीर और मस्तिष्क में होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना लगभग असम्भव है । इसलिए प्राणायाम को किसी अनुभवी गुरु के विशेष निर्देशन में ही किया जाना चाहिए ।
क्योंकि प्राणायाम में कितनी गति दी जाय यह अभ्यासी व रोगी के स्वभाव पर निर्भर करता है , इसका निर्धारण गुरु ही करता है किताब नहीं ।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy