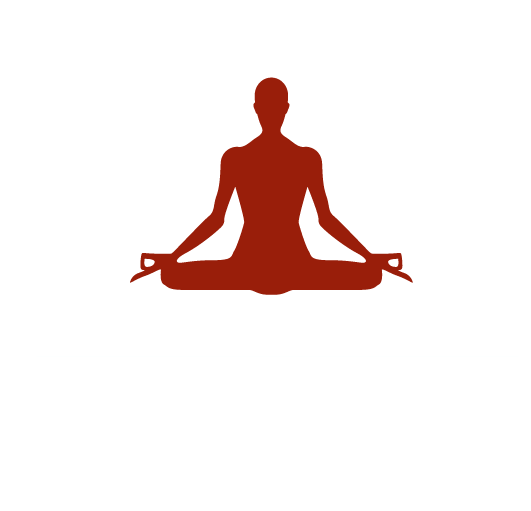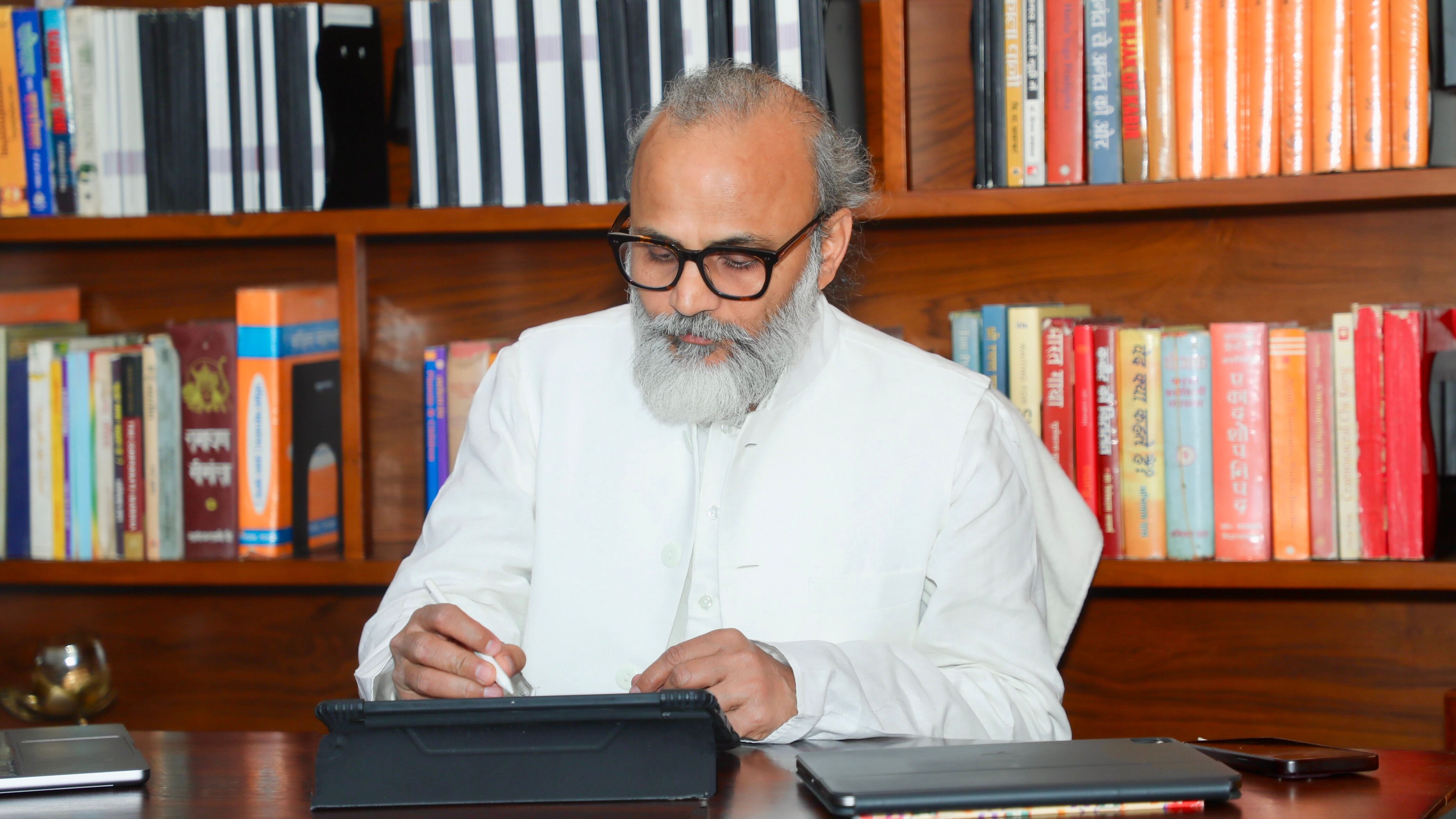
ऐच्छिक गति: नियंत्रण
11 months ago By Yogi Anoopऐच्छिक गति: नियंत्रण और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय
हमारे जीवन में गति अनिवार्य है। ऐच्छिक गति (Voluntary Motion) को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को बचाने का एक अनिवार्य तत्व है । ठीक उसी प्रकार जैसे भोजन करते समय मुँह की चबाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है, वैसे ही सामान्य जीवन में भी कर्म को पूरी तरह नष्ट करना संभव नहीं । जीवन सतत प्रवाहमान है, और गति इस प्रवाह का मूल आधार है ।
लेकिन क्या गति केवल एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, या इसे किसी उच्चतर स्तर पर नियंत्रित किया जा सकता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर हमें योग, ध्यान और भारतीय दर्शन में मिलता है। गति को समाप्त किए बिना इसे संयमित करना ही आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में पहला कदम होता है। चूँकि यह गति ऐक्षिक क्रिया के द्वारा पैदा है इसलिए इस गति को कम या अधिक किया जा सकता है । इसी गति के तीव्र होने पर तनाव, अवसाद और फ्रस्ट्रेशन इत्यादि पैदा होता है । और इसकी गति को धीरे करने पर ऐक्षिक गति के नियंत्रण कर्ता को स्थिरता की अनुभूति होती है ।
गति को रोकने का प्रयास या उसका रूपांतरण?
संसार में बहुत से लोग गति को रोकने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि कर्म या किसी भी प्रकार की गति से पूरी तरह विरक्त होकर ही वे शांति प्राप्त कर सकते हैं। किंतु क्या यह वास्तव में संभव है? यदि हम गहराई से विचार करें, तो पाएंगे कि गति को रोकना प्राकृतिक नहीं है। मन और इन्द्रियों के द्वारा किया गया किसी भी क्रिया में हो रहे गति को रोकने के बजाए , उसमें लयबद्धता लानी आवश्यक होती है । इसे एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं:
जब भोजन कर रहे होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुँह चबाने की प्रक्रिया में लगा रहता है। क्या इसे रोका जा सकता है? बिल्कुल नहीं! किंतु एक महत्वपूर्ण परिवर्तन तब होता है जब हम भोजन के स्वाद को पूरी तरह से अनुभव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही भोजन करने वाले का ध्यान स्वाद की अनुभूति में डूब जाता है, वैसे ही चबाने की गति स्वाभाविक रूप से धीमी और नियंत्रित हो जाती है। यहाँ पर गति को बिना रोके उसे रूपांतरित करने का सर्वोत्तम उदाहरण है । मैं इसी को गति पर नियंत्रण कहता हूँ ।
गति में नियंत्रण और ध्यान का प्रभाव
इस परिप्रेक्ष्य में गति का नियंत्रण ही ध्यान की पहली अवस्था है। किसी कार्य में संलग्नता की अनुभूति ही उस कार्य की गति को सहज बना देती अहि और साथ साथ यांत्रिक क्रिया से परे कर देती है । यही अनुभव सजगता और धैर्य भी स्वतः पैदा कर देती है । इसी अनुभूति से स्थिरता का बोध भी होता है । यही कारण है कि योग और ध्यान में ‘सजगता पूर्ण अनुभूति’ (Awareness) पर अत्यधिक बल दिया जाता है।
जब व्यक्ति किसी भी गति को केवल बाह्य गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति के रूप में देखता है, तो वह गति स्वतः ही संतुलित हो जाती है । गति को नियंत्रित करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए । यह संतुलन ही आत्मनियंत्रण का मूल रूप है। इसे ध्यान के उच्च स्तर पर ले जाया जाए तो व्यक्ति कर्म में लिप्त होते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है।
कर्म में निष्कामता: गति और स्थिरता का अद्भुत संतुलन
इस उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय दर्शन में ‘कर्म में निष्कामता’ का सिद्धांत इसी गति और स्थिरता के संतुलन से उत्पन्न हुआ । कर्म की गति बनी रहती है, किंतु कर्म की गति व चक्र में फँस कर तनाव और रोग नहीं लेता । यह वही अवस्था है जिसे श्रीकृष्ण ने गीता में ‘निष्काम कर्म’ कहा है—
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।”
(तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं।)
इस भाव का अर्थ यह नहीं है कि कर्म के फल की इक्षा ही छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि कर्म करते समय ही कर्म के द्वारा जो फल तुरंत अनुभव हो रहा है उस पर ध्यान देना । कर्म करते समय प्राप्त होने वाला अनुभव ही कर्म की गति से परे की अनुभूति है । यही निष्कामता है ।
भारतीय दर्शन में भी इस गति के विज्ञान का महत्व छिपा हुआ है । दार्शन की इस परंपरा में गति केवल भौतिक ऐक्षिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह चेतना की अवस्था से भी जुड़ी हुई है। जब गति को बाहरी नियंत्रण से नहीं, बल्कि गति के मूल केंद्र में जाकर उसकी स्थिरता की अनुभूति से संयमित किया जाता है, तो वह ध्यान का रूप ले लेती है। यही ध्यान व्यक्ति को उसके आत्मबोध की ओर ले जाता है।
यदि इस अवधारणा को गहराई से समझें, तो पाएंगे कि गति और स्थिरता वास्तव में परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे एक-दूसरे के पूरक हैं। स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं है, और गति का अर्थ अराजकता नहीं है। एक नियंत्रित गति ही वास्तविक स्थिरता प्रदान कर सकती है। यही कारण है कि योग और ध्यान में इस सिद्धांत को गहराई से अपनाया गया है।
संक्षेप में, ऐच्छिक गति को पूरी तरह से रोकना न केवल असंभव है, बल्कि यह आवश्यक भी नहीं है। गति को रोकने के बजाय, स्वयं के द्वारा गति के मूल का अनुभव करके रूपांतरित करना ही वास्तविक साधना है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण सजगता और धैर्य के साथ किसी भी क्रिया में संलग्न होता है, तो वह क्रिया ध्यान का रूप ले लेती है। यही ध्यान व्यक्ति को कर्म के बंधन से मुक्त कर सकता है और उसे निष्काम कर्म के पथ पर अग्रसर कर सकता है।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy