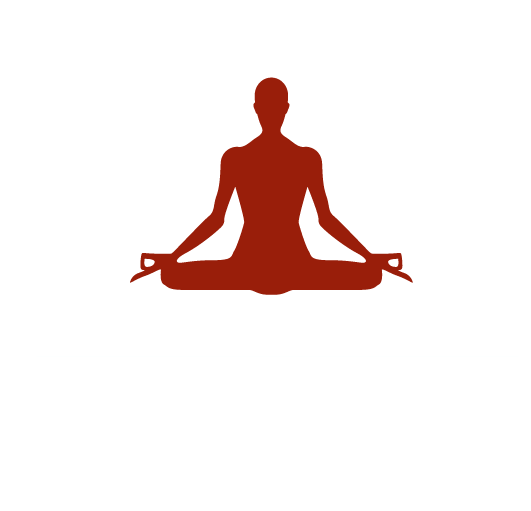आसक्ति से पेट के रोग
1 year ago By Yogi Anoopआसक्ति से पेट के रोग: मन और मस्तिष्क को संतुलन में लाने का मार्ग ; योगी अनूप और शिष्य के बीच संवाद
शिष्य: गुरुजी, मन किसी विचार या वस्तु से इतनी जल्दी आसक्त क्यों हो जाता है? क्या यह स्वाभाविक है, और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है?
योगी अनूप: बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वभाव के अनुरूप मन रुचि के अनुरूप किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाता है। यही आकर्षण ही उसकी आसक्ति बन बैठती है । जब आप किसी पवित्र विचार, लक्ष्य, या वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मन की प्रवृत्ति उस ओर खिंचने की होती है। इससे मन में अन्य असंगत या अनावश्यक वस्तुओं की चाहत धीरे-धीरे कम हो जाती है।
यह प्रक्रिया उसी तरह काम करती है जैसे किसी को भोजन के एक विशेष स्वाद की आदत लग जाती है। एक बार जीभ को किसी स्वाद का चस्का लग गया, तो अन्य स्वाद उसे उतने रुचिकर नहीं लगते। वह इसलिए कि मन अपने रुचिकर विषय से मस्तिष्क के अंदर उस विशेष स्वाद के प्रति आदत बना चुका हुआ होता है । यूँ कहे कि वह आदत उसकी लत के समान हो चुकी हुई होती है । यहीं से उसकी समस्या का प्रारंभ होता है ।
शिष्य: गुरुजी, तो क्या यह कहना सही होगा कि मन को किसी एक विचार या आदत का आदी बनाना एक प्रकार का समाधान है?
योगी अनूप: आसक्ति को समाधान समझना एक बड़ा भ्रम है। एक आदत को हटाने के लिए किसी दूसरी आदत का निर्माण कर लेना एक सीमा तक उचित है और यह एक तात्कालिक उपाय तो हो सकता है, किंतु दीर्घकाल में यह समस्या को रोगों में परिवर्तित करके और गहराई में ले जा सकता है। किसी एक विचार या आदत की लत लगने से मन अपने स्वाभाविक संतुलन को खो देता है। और उस संकीर्ण दृष्टिकोण से मन इतना अधिक असंतुष्ट हो जाता है कि भविष्य में वह ऐसे ऐसे कार्य करने लगता है जिसे वह कल्पना भी नहीं कर सकता है ।
इसलिए इसे समाधान के रूप नहीं देखना चाहिए । बस एक तात्कालिक समस्या से बचने के उपाय के रूप में ही देखे । इस उपाय से मस्तिष्क के अंदर उन न्यूरॉन्स में बदलने की ताक़त का अवश्य निर्माण होता है । उनके अंदर बदलाव की शक्ति भी आती है किंतु किसी एक आदत में निरंतरता से चिपक जाने से दीर्घकालीन में समस्या व रोगों का आना निश्चित ही है ।
ध्यान दें इसका अर्थ यह नहीं कि बुरी आदत को त्यागने के लिए अच्छी न आदत बनायें और फिर अच्छी आदत को भी त्यागने के लिए कोई और आदत बनाये । इसका मूल अर्थ है आदत के पीछे के रहस्यों को समझें , उसे अनुभव करें , उसकी गहराई में जायें । तो उस कार्य को करते हुए भी किसी आदत से आसक्त नहीं होंगे ।
शिष्य: तो गुरुजी, आसक्ति के कारण मन और मस्तिष्क का संतुलन क्या बिगड़ जाता है?
योगी अनूप: आसक्ति के मूल में यह है कि आप अपने मन को बिना विवेक के किसी एक दिशा में आवश्यकता से अधिक मोड़ कर अति कर देते हैं । चूँकि इसमें एकाग्रता बिना विवेक के , बिना समझे की जाती है इसलिए इसमें मन को रोकने का ज्ञान नहीं हो पाता है और यही कारण है कि वह बाकी दिशाओं को अनदेखा कर देता हैं। और मस्तिष्क का कोई एक विशेष हिस्सा आवश्यकता से अधिक कार्य करने लगने से मस्तिष्क के अन्य हिस्से अछूते रह जाते हैं । किंतु व्यावहारिक जीवन में हर दिशा का महत्व है। जब आप केवल एक दिशा में मन को बांधते हैं, तो वह स्वाभाविक संतुलन खो बैठता है।
मस्तिष्क और मन का संतुलन जीवन के हर व्यवहार पहलू के लिए आवश्यक है। यदि यह संतुलन नहीं होगा, तो आपका मस्तिष्क एक ही विचार में उलझा रहेगा। इसके परिणामस्वरूप, आपकी स्वतंत्र सोच समाप्त हो सकती है। और जहां स्वतंत्रता समाप्त होती है, वहीं से मानसिक तनाव, असंतोष और गलत निर्णय शुरू होते हैं।
शिष्य: गुरुजी, इसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या यह व्यक्ति के विकास को रोक सकता है?
योगी अनूप: बिल्कुल। आसक्ति का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह व्यक्ति को एक सीमित दायरे में बांध देती है। आप केवल उसी विचार, वस्तु, या आदत पर निर्भर हो जाते हैं। इससे आपका मानसिक विकास रुक जाता है।
• आंतरिक संघर्ष: जब मन केवल एक चीज़ में बंध जाता है, तो बाकी इच्छाएँ उसे परेशान करने लगती हैं। यह मानसिक संघर्ष पैदा करता है।
• निर्णय की क्षमताओं में गिरावट: एक विचार में उलझे रहने से आप विभिन्न परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं।
• शारीरिक और मानसिक तनाव: आसक्ति से उत्पन्न असंतोष आपके शरीर और मस्तिष्क दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है ।
शिष्य: तो फिर गुरुजी, इसका सही समाधान क्या है?
योगी अनूप: समाधान संतुलन में है। संतुलन का मतलब है कि आप अपने मन और मस्तिष्क को किसी एक विचार में बांधने के बजाय, उन्हें स्वतंत्र और स्थिर रखें। संतुलन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:
1. विविधता को स्वीकार करें: जीवन में केवल एक विचार या आदत तक सीमित न रहें। विभिन्न विचारों और अनुभवों को अपनाएँ।
2. ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें: ध्यान मन को शांत करता है और उसे अस्थिरता से बचाता है।
3. स्वतंत्रता का अभ्यास करें: अपने मन को स्वतंत्र रूप से सोचने दें। जब मन किसी एक विचार में उलझे, तो उसे पहचानें और उसे छोड़ने का प्रयास करें।
4. अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करें: यह समझने की कोशिश करें कि आपकी इच्छाएँ आपको कैसे प्रभावित कर रही हैं।
Recent Blog
Copyright - by Yogi Anoop Academy